सी. एन. सुब्रह्मण्यम
कुछ दिन पहले मैंने अपने देश के अग्रणी भाषाविद सुनीति कुमार चटर्जी का एक बहुत ही दिलचस्प लेख पढ़ा। इस लेख में कई ऐसी बातें हैं जो हमारे इतिहास के राजनैतिक, भाषाई, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को छूती हैं। सोचा कि संदर्भ के पाठक भी इसका लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन यह सुनीति बाबू के लेख का अनुवाद नहीं है, बल्कि एक रूपांतरण है।
औरंगजेब के जमाने के इतिहास कारों में से मुहम्मद साकी मुस्तअद काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मआथिर-ए-आलमगीरी नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन है। बात 1690 ईसवी की थी जब औरंगजेब देकन में कृष्णा नदी के किनारे दौरे पर था। घटना का वर्णन मआथिर-ए-आलमगीरी में इस प्रकार है।
एक दिन जब बादशाह अपनी अदालत में बैठे थे तो सलाबत खान ने एक आदमी को पेश किया; उसे व्यक्ति ने कहा, “मैं दूर बंगाल से आया हूं ताकि आलमपनाह का मुरीद ( शिष्य ) बन सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मुराद पूरी करेंगे।'' बादशाह उसकी बात पर मुस्कुराए; उन्होंने अपनी जेब से सौ रुपए और सोने व चांदी के टुकड़े निकालकर यह कहते हुए सलाबत खान को दिए कि,
उससे कहो कि जो मुराद वह मुझसे चाहता है वह यही है।'' उस बंगाली व्यक्ति ने बादशाह के दिए हुए उन रुपयों आदि को फेंक दिया और अचानक पास बह रही कृष्णा नदी में कूद गया। खूब हो-हल्ला हुआ और बादशाह के आदेश पर कुछ लोगों ने पानी में से उसे निकाला। बादशाह ने अपने साथियों की तरफ मुड़कर कहा, यह बंदा बंगाल से इस मूर्खतापूर्ण
विचार को लेकर आया है कि वह मेरा मुरीद बनेगा!'' यह कहने के साथ साथ बादशाह ने एक हिंदवी दोहा भी सुनाया।''
टवपी लिंड़ी बवरी दिंदी खरे नलज।
चवह खदन मवली तव कल बनधी छज॥
इस दोहे को भी मआथिर में दिया गया है लेकिन फारसी लिपि में। फारसी लिपि में स्वरों के लिए मात्राओं का प्रयोग एक खास तरीके से होता है। या फिर अक्सर होता ही नहीं है। पाठक संदर्भ के अनुसार खुद मात्रा लगाकर पढ़ते जाते हैं। तो फारसी में दोहे का जो हाल हुआ देखिएः
कई इतिहासकारों ने इस दोहे का अर्थ निकालने का प्रयास किया लेकिन वे संदर्भ से मेल नहीं खा रहे थे। औरंगजेब के आधुनिक इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इसका अर्थ इस प्रकार निकालाः टोपी लेंदे बावरे देदे खरे निलाज। चूहा खादन मावली तू कल बंधे छज॥ आज की भाषा में इसका अर्थ होगा, ‘ओ बावरे तुम टोपी पहनकर बावड़ी खोदने की बात करते हो? चूहे तेरे घर की नींव खोद रहे हैं और तू कल के लिए छज्जा बना रहे हो?”
जाहिर है उस खास मौके पर औरंगज़ेब ने इस तरह के एक दोहे को
क्यों कहा होगा यह समझ में नहीं आता है।
सुनीति बाबू ने अपने शोध के दौरान इस पर विचार किया था और उन्होंने एक और विवेचना की। लेकिन वह भी संतोषजनक नहीं थी। इसी बीच एक दिन गुरू ग्रंथ साहब का अध्ययन करते वक्त उन्हें इस दोहे से मिलता-जुलता एक दोहा दिखा। दोहे के रचयिता थे स्वयं गुरू नानक।
"कुल्हां देदे बावरे लैंदे वडे निलज।
चूहा खड' न मावई तिकलि बंन्दै छज॥''
यानी,
बावरे कुल्हा देते हैं ( मुरीदी की टोपी पहनाकर शिष्य बनाते हैं) और निर्लज्ज लोग उन्हें स्वीकार करते हैं।
चूहा खुद तो छेद ( खड) के अंदर नहीं घुस पा रहा है पर उसने अपने पीठ पर एक सुपे को बांध रखा है।
आप देख सकते हैं कि अब अर्थ संदर्भ में सही रूप में बैठ रहा है। औरंगजेब यह कह रहा था कि हर कोई गुरू होने का दावा नहीं कर सकता है और जो खुद को पार नहीं लगा सकता है वह दूसरों को कैसे पार लगाएगा? शायद वह खुद की कमजोरियों पर गौर कर रहा था।
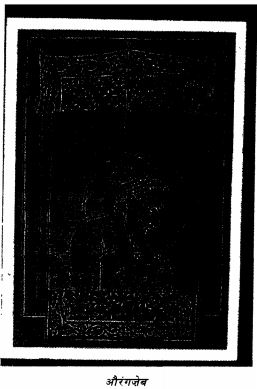 फिर सुनीति बाबू यह सवाल उठाते हैं कि नानक का यह दोहा औरंगजेब की जुबान में कैसे आया? उसने तो सिखों को खतम करने की ठानी थी।
फिर सुनीति बाबू यह सवाल उठाते हैं कि नानक का यह दोहा औरंगजेब की जुबान में कैसे आया? उसने तो सिखों को खतम करने की ठानी थी।
यह संभावना कम ही लगती है। कि उसने ग्रंथ साहब का अध्ययन किया हो। अगर उसे पता होता कि इसके रचयिता गुरू नानक हैं तो शायद वह उसका उपयोग ही न करता! यह दोहा बोलचाल में प्रचलित हुआ होगा। यानी कि जिस तरह लोग कबीर और रहीम के दोहों को अनायास ही उपयोग करते हैं वैसे ही इस दोहे का भी उन दिनों प्रचलन रहा हागा। लेकिन सवाल अभी
भी बचता है कि यह दोहा औरंगजेब तक कैसे पहुंचा?
अब कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है - सुनीति बाबू मुगल शाही परिवार में इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं की खोज में निकल पड़ते हैं। शाही परिवार के सदस्य किस बोली में बोलते होंगे?
बाबर की मातृ भाषा तो तुर्की थी। वह उस भाषा मे बखूबी बोलता था और लिखता पढ़ता भी था। उसके
बाद उसके वंशज - जो भारत में बस गए थे - धीरे-धीरे तुर्की भूलते गए। ( औरंगजेब अपने बेटे को लिखे गए खत में इस बात पर नाराजगी जाहिर करता है कि वह अपने तुर्की पढ़ाने वाले उस्ताद को चकमा देकर भाग जाता है।)
एक तो उन्होंने फारसी भाषा को अपनाया जो उस वक्त शासन करने के लिए जरूरी थी। लेकिन रोज़ उठते बैठते, आपस में बतियाने के लिए वे धीरे-धीरे ब्रजभाषा और तत्कालीन खड़ी बोली को अपनाने लगे। ये बोलियां आगरा और देहली की स्थानीय बोलियां थीं। याद कीजिए कि ‘अब्दुल रहीम', 'बैरम खान' का पुत्र था और अकबर ने उसे अपने पुत्र के समान शाही महल में पाला था। रहीम ब्रजभाषा के सर्वोत्तम कवियों में माने जाते हैं। अकबर खुद ब्रज में कविताएं रचता था। शाही परिवार में पिता को ‘बाबाजी' कहते थे न कि अब्बा जान। भाई एक दूसरे को 'दादा' या 'भाई' करके पुकारते थे।
पश्चिमी भारत में ब्रज के अलावा एक तरह की खड़ी बोली भी बोली जाती थी, जो साधुओं, सूफियों, फकीरों और जोगियों के द्वारा उपयोग की
जाती थी। उन दिनों उसे ‘साधुककड़ी' बोली कहते थे। इसी बोली के माध्यम से तुकाराम, कबीर, नानक, दादू और रैदास जैसे भक्तों के दोहे और पद जनसामान्य के बीच फैले। सुनीति कुमार का कहना है कि मुगल राजवंश के लोगों ने इन बोलियों को, अपने संपर्क में आने वालों से सीखा होगा और इनके माध्यम से वे भक्तों के इन दोहों से परिचित हुए होंगे।
ब्रज और खड़ी बोली के अलावा सुनीति कुमार बताते हैं कि शाही परिवारों में कुछ संस्कृत का ज्ञान भी अपेक्षित था। वे बताते हैं कि यह परंपरा थी कि सारे हाथियों के नाम संस्कृत में हों और सारे घोड़ों के नाम फारसी में। शायद समझ यह थी कि जो हिंदुस्तान की चीज़ है उसका नाम संस्कृत में और जो अरब या ईरान से आते थे उनका नाम फारसी में होना चाहिए। सुनीति कुमार एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं : एक बार एक शहज़ादे ने औरंगजेब को दो नए किस्म के आम भेजे और उससे उनके लिए नाम सुझाने के लिए कहा।
औरंगजेब ने एक को ‘सुधा रस' नाम दिया और दूसरे को ‘रसना विलास'
- दोनों परिष्कृत संस्कृत नाम हैं।
सी. एन. सुब्रह्मण्यम: एकलव्य के सामाजिक अध्ययन शिक्षण कार्यक्रम से संबद्ध।
संदर्भ: S.K.Chatterjee, 'A verse by Guru Nanak in Adi Granth Quoted by Emperor Aurangazeb Alamgir' Select Papers VoIIIPPH New Delhi 1979.



