प्रेमपाल शर्मा
 एन.सी.ई.आर.टी. ने कुछ वर्ष पहले ‘समझ का माध्यम’ पर राष्ट्रीय बहस, विचार विमर्श की शुरुआत कर शिक्षा के सन्दर्भ में बहुत सार्थक पहल की थी। वास्तव में सही शिक्षा वही मानी जा सकती है जो समझ का विकास करे और समझ के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण औज़ार है। यानी कि अगर अपनी भाषा में पढ़ाई-लिखाई हो तो पढ़ने का आनन्द तो आता ही है साथ ही अपने परिवेश, ज्ञान, विज्ञान की सच्ची समझ भी इसी रास्ते आती है। दुनिया के हर बड़े चिन्तक, मनीषियों और शिक्षाविदों ने बार-बार यही बात दोहराई है।
एन.सी.ई.आर.टी. ने कुछ वर्ष पहले ‘समझ का माध्यम’ पर राष्ट्रीय बहस, विचार विमर्श की शुरुआत कर शिक्षा के सन्दर्भ में बहुत सार्थक पहल की थी। वास्तव में सही शिक्षा वही मानी जा सकती है जो समझ का विकास करे और समझ के लिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण औज़ार है। यानी कि अगर अपनी भाषा में पढ़ाई-लिखाई हो तो पढ़ने का आनन्द तो आता ही है साथ ही अपने परिवेश, ज्ञान, विज्ञान की सच्ची समझ भी इसी रास्ते आती है। दुनिया के हर बड़े चिन्तक, मनीषियों और शिक्षाविदों ने बार-बार यही बात दोहराई है।
मैं अपनी बात कुछ अनुभवों को सामने रखकर स्पष्ट करना चाहूँगा।
अपने पड़ोस में एक ऐसे बच्चे को मैं जानता हूँ जिसे बहुत सिफारिशों के बाद एक निजी स्कूल में दाखिला मिल पाया। लेकिन अफसोसजनक स्थिति यह रही कि कई साल के धैर्य के बावजूद बच्चे की पढ़ाई-लिखाई, या स्कूल में रुचि की प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही। नवीं तक आते-आते बच्चा फेल होने की कगार पर आ गया। मैं भी इस दौरान दो-चार बार स्कूल गया, अध्यापकों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी। जो कारण समझ आया वह था कि दिल्ली के 99% निजी स्कूलों का माध्यम अँग्रेज़ी है पर बच्चा अँग्रेज़ी ठीक ढंग से न तो समझ पाता है और न अपनी बात कह पाता है। मैं बच्चे से बार-बार एक ही बात पूछता था कि “क्या तुम क्लास में कोई प्रश्न पूछते हो?” मेरे बार-बार उकसाने के बावजूद और शिक्षकों के विशेष रूप से प्रश्न पूछने की ओर ध्यान दिलाने के बावजूद बच्चे में वह हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं बन पा रहा था कि यदि कोई बात समझ में न आए तो उसे वह अध्यापक से पूछ ले। निजी स्कूल हों या देश के ज़्यादातर सरकारी स्कूल, उनकी शिक्षा-पद्धति में प्रश्न पूछने को कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। शायद हमारे धर्म या संस्कारों में ही ऐसा कुछ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष गोद दिया जाता है कि बड़ों के सामने प्रश्न नहीं करते। यानी बड़ों, सम्माननीयों ने, स्कूल के अर्थ में शिक्षक, गुरूजी, सर ने जो कह दिया, बस वही ठीक है। कहीं आगे चलकर नौकरशाही की ‘यस सर’ इसी का विस्तार तो नहीं है? बच्चे साल-दर-साल बहुत गम्भीरता से मूर्ति बने प्रवचन सुनते रहेंगे लेकिन क्लास के तुरन्त बाद उनकी खुसर-फुसर, बातचीत और ठहाके ये बताते हैं कि उन्होंने कितनी बन्दिशों में स्कूल में समय बिताया है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शायद इसी पक्ष को रेखांकित करते हुए कहा था, “बच्चे सरस्वती के मन्दिर में मज़दूरी करते हुए अपना बचपन बिता देते हैं।”
खैर, मैं लौटकर अपनी बात पर आता हूँ। ऐसा बच्चा जो न प्रश्न पूछ सकता है और न क्लास में बोल सकता है वह धीर-धीरे पिछड़ता तो जाएगा ही, और ऐसे गड्ढे में धकेल दिया जाएगा कि स्कूल या शिक्षा से बाहर ही हो जाए। निजी स्कूली संस्थाओं में शायद ही किसी के पास इतना धैर्य हो कि वह ऐसे पिछड़ते बच्चे की तरफ ध्यान दे। इन स्थितियों में गणित और विज्ञान में बच्चे की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर बनी हुई थी। अच्छी तो सामाजिक विज्ञान और अँग्रेज़ी में भी नहीं थी लेकिन हिन्दी में ठीक अंक मिल रहे थे क्योंकि यह उसके घर पर अपेक्षाकृत कम पढ़े-लिखे माँ-बाप और समाज की भाषा थी।
मुझे एक तरकीब सूझी। मुझे लगा कि यदि इस बच्चे को इस निजी तथा कथित प्रसिद्ध स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिल करा दिया जाए जहाँ पढ़ाई का माध्यम अपनी भाषा यानी हिन्दी होता है तो शायद बात बन जाए। सात-आठ कि.मी. दूर आने-जाने का समय और फीस तो बचेगी ही।
मैंने उसे उस स्कूल से निकालने का सुझाव दिया। पहले तो माँ-बाप बिलकुल तैयार ही नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद वे तैयार भी हुए तो उनके पड़ोस के लोगों ने उन्हें डरा दिया कि सरकारी स्कूल भी कोई स्कूल होते हैं। वहाँ तो कामवालियों के बच्चे पढ़ते हैं, गाली सीखते हैं, न पढ़ने की जगह होती है, न ही अध्यापक आते हैं, न कोई ड्रेस-टाई, न तहज़ीब। वहाँ जाकर तो बच्चा और बिगड़ जाएगा। इन सामाजिक दबावों के चलते 9वीं में भी बच्चा उसी निजी स्कूल में बना रहा और बमुश्किल चालीस प्रतिशत अंक लेकर पास हो पाया। 10वीं कक्षा अप्रैल से शु डिग्री हो गई थी। गर्मियों में बच्चे की ट्यूशन भी हुई लेकिन जुलाई के पहले हफ्ते में जब टेस्ट के रिज़ल्ट आए तो इस बार भी उतने ही निराशाजनक थे जितने कि पिछले दो-तीन सालों में। इस बार सलाह के नाम पर मेरा फैसला बहुत स्पष्ट था -- जितनी जल्दी हो बच्चे का दाखिला तथाकथित अँग्रेज़ी निजी स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में करा दिया जाए वरना बच्चे का पास होना ही दूभर हो जाएगा।
 स्कूल की तलाश शुरू हुई। घर के पास दो सरकारी स्कूल थे। दोनों लगभग आधे किलोमीटर से भी कम के फासले पर। यहाँ सरकारी स्कूल-व्यवस्था का एक और रूप सामने आया। मैं नज़दीक, एक फर्लांग पर स्थित स्कूल में खुद गया। एक कक्षा में सिर्फ 20-22 बच्चे थे। जबकि होने चाहिए थे 40 से 50। प्राचार्य महोदय के नखरे देखने लायक थे। बजाए इसके कि वे और बच्चों का स्वागत करें, उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मैं उनका समय बरबाद कर रहा हूँ। “आप तो पढ़े-लिखे हैं, इतने अच्छे स्कूल को छोड़कर बच्चे को यहाँ क्यों लाना चाहते हैं?” उन्होंने आशंका प्रकट की कि कहीं बच्चा फेल तो नहीं हो गया या सिर्फ ले-देकर पास कर दिया हो। “इस बार तो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप लेट हो गए हैं।” मेरी इस बात का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा कि “सरकारी स्कूल आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए होते हैं और आपकी क्लास में बच्चे भी बहुत कम हैं।” लेकिन वे नहीं माने। खैर मैं दूसरे सरकारी स्कूल में दाखिला कराने में सफल हो गया।
स्कूल की तलाश शुरू हुई। घर के पास दो सरकारी स्कूल थे। दोनों लगभग आधे किलोमीटर से भी कम के फासले पर। यहाँ सरकारी स्कूल-व्यवस्था का एक और रूप सामने आया। मैं नज़दीक, एक फर्लांग पर स्थित स्कूल में खुद गया। एक कक्षा में सिर्फ 20-22 बच्चे थे। जबकि होने चाहिए थे 40 से 50। प्राचार्य महोदय के नखरे देखने लायक थे। बजाए इसके कि वे और बच्चों का स्वागत करें, उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि मैं उनका समय बरबाद कर रहा हूँ। “आप तो पढ़े-लिखे हैं, इतने अच्छे स्कूल को छोड़कर बच्चे को यहाँ क्यों लाना चाहते हैं?” उन्होंने आशंका प्रकट की कि कहीं बच्चा फेल तो नहीं हो गया या सिर्फ ले-देकर पास कर दिया हो। “इस बार तो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, आप लेट हो गए हैं।” मेरी इस बात का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ा कि “सरकारी स्कूल आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए होते हैं और आपकी क्लास में बच्चे भी बहुत कम हैं।” लेकिन वे नहीं माने। खैर मैं दूसरे सरकारी स्कूल में दाखिला कराने में सफल हो गया।
आप यकीन मानिए, दिसम्बर तक आते-आते 6 महीने के अन्दर ही बच्चे का आत्मविश्वास लौट आया और दसवीं की परीक्षा में वह 70% अंकों से पास हुआ और क्लास में अव्वल भी रहा। नि:सन्देह हर बच्चे में प्रतिभा होती है, बशर्ते उसको फलने-फूलने, अपने परिवेश, अपनी भाषा में सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिले। यहाँ स्कूल में अपनी भाषा यानी कि हिन्दी में पढ़ने-पढ़ाने के बूते, आत्मविश्वास के करिश्मे का उदाहरण है यह शैक्षिक अनुभव।
एक और अनुभव
एक बच्चे की फुटबाल खेलते-खेलते पैर की हड्डी टूट गई और डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया। और प्लास्टर भी चार महीने के लिए, पंजे से लेकर जांघ तक। उन्हीं दिनों दसवीं के फॉर्म भरे जा रहे थे। यह छात्र चलने-फिरने में असमर्थ एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। सभी के चेहरों पर दसवीं के बोर्ड का आतंक था। बातचीत से पता लगा कि यह बच्चा सामाजिक विज्ञान जैसे विषय की समझ तो अच्छी रखता है, लेकिन उसे अँग्रेज़ी में लिखने में दिक्कत होती है। यह लड़का केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ता था। मैंने सुझाव दिया कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हिन्दी में ही दे तो अच्छा रहेगा। यह मेरे अकेले का अनुभव नहीं, यह तो हम सबका अनुभव है कि विज्ञान या गणित के प्रश्नों के उत्तर तो एक बार को अँग्रेज़ी माध्यम में दिए जा सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के उत्तर देने में अपनी भाषा का आनन्द है, लेकिन यहाँ भी स्कूली व्यवस्था का एक और चेहरा सामने था। उनका कहना था कि यदि नवीं कक्षा में अँग्रेज़ी माध्यम है तो दसवीं कक्षा में भी सामाजिक विज्ञान विषय का माध्यम अँग्रेज़ी ही रखना पड़ेगा, जबकि हकीकत में ऐसा कोई नियम नहीं है। बच्चे ने सामाजिक विज्ञान की परीक्षा हिन्दी माध्यम में दी और बहुत अच्छे यानी 86% अंक प्राप्त किए।
इन दोनों अनुभवों से मैंने यह कहने की कोशिश की है कि सामान्य-से-सामान्य विद्यार्थी यदि विषयों को अपनी भाषा में समझ ले तो कई गुना बेहतर प्रदर्शन करता है।
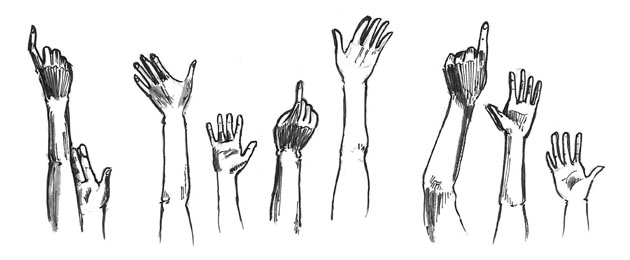 क्या एन.सी.ई.आर.टी. समेत पूरी शिक्षा व्यवस्था और हम सब इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर सोचते हुए कई बार एक अन्धेरे में घिरता हुआ महसूस करता हूँ। जो अँग्रेज़ी स्कूल खुल रहे हैं उनमें अँग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तकें कौन-सी हैं और क्या अँग्रेज़ी के इतने शिक्षक उपलब्ध हैं? शिक्षाविद् कृष्ण कुमारजी की दो-तीन दशक पहले लिखी बात का सहारा लें तो उन्होंने कहा था कि “जो शिक्षक हमें अँग्रेज़ी पढ़ाते हैं यदि उनकी अँग्रेज़ी ठीक होती तो वे पहले ही कहीं और नौकरी कर रहे होते। अब इन अक्षम अँग्रेज़ी शिक्षकों से जो अँग्रेज़ी पढ़ने को मिलेगी उसका स्तर भी वही होगा जो आज है।” यदि मामला सिर्फ अँग्रेज़ी को एक विषय के रूप में पढ़ाने का हो तब भी बात समझ में आती है। लेकिन बात तो यहाँ तक बढ़ रही है कि प्राइमरी की शिक्षा भी अँग्रेज़ी माध्यम में देने की वकालत की जा रही है और इसमें कई राज्य एक-दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं। चुनौती बड़ी ज़रूर है, लेकिन असम्भव नहीं, वरना शिक्षा समझ के माध्यम के बिना निरर्थक ही रहेगी।
क्या एन.सी.ई.आर.टी. समेत पूरी शिक्षा व्यवस्था और हम सब इन चुनौतियों के लिए तैयार हैं? इस प्रश्न पर सोचते हुए कई बार एक अन्धेरे में घिरता हुआ महसूस करता हूँ। जो अँग्रेज़ी स्कूल खुल रहे हैं उनमें अँग्रेज़ी की पाठ्यपुस्तकें कौन-सी हैं और क्या अँग्रेज़ी के इतने शिक्षक उपलब्ध हैं? शिक्षाविद् कृष्ण कुमारजी की दो-तीन दशक पहले लिखी बात का सहारा लें तो उन्होंने कहा था कि “जो शिक्षक हमें अँग्रेज़ी पढ़ाते हैं यदि उनकी अँग्रेज़ी ठीक होती तो वे पहले ही कहीं और नौकरी कर रहे होते। अब इन अक्षम अँग्रेज़ी शिक्षकों से जो अँग्रेज़ी पढ़ने को मिलेगी उसका स्तर भी वही होगा जो आज है।” यदि मामला सिर्फ अँग्रेज़ी को एक विषय के रूप में पढ़ाने का हो तब भी बात समझ में आती है। लेकिन बात तो यहाँ तक बढ़ रही है कि प्राइमरी की शिक्षा भी अँग्रेज़ी माध्यम में देने की वकालत की जा रही है और इसमें कई राज्य एक-दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं। चुनौती बड़ी ज़रूर है, लेकिन असम्भव नहीं, वरना शिक्षा समझ के माध्यम के बिना निरर्थक ही रहेगी।
प्रेमपाल शर्मा: रेलवे बोर्ड में संयुक्त सचिव हैं। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में लम्बे समय से लेखन। शिक्षा के प्रचार-प्रसार में गहरी रुचि। दिल्ली में निवास।
सभी चित्र: किरन जोन: चित्रकला परिषद, बेंगलुरु की छात्रा हैं। मूर्तिकला में स्पेशलाइज़ेशन कर रही हैं। बच्चों के लिए चित्रकारी करने में रुचि।



