मनीष
साक्षात्कार
 प्रश्न - आज के समय में आधुनिक शिक्षा गाँव को किस प्रकार प्रभावित कर रही है?
प्रश्न - आज के समय में आधुनिक शिक्षा गाँव को किस प्रकार प्रभावित कर रही है?
इस प्रभाव पर चर्चा करने से पहले हमें आधुनिक शिक्षा के अर्थ को समझना होगा। जिसे हम आधुनिक शिक्षा कह रहे हैं, वो मुख्यत: इस प्रवृत्ति को जन्म देती है कि मैं जहाँ हूँ, वहाँ से चला जाऊँ। शिक्षा की पाठ्यचर्या, शिक्षा का अर्थव्यवस्था के साथ सम्बन्ध और ऐतिहासिक रूप से जो औपनिवेशिक दौर में गाँव और शहर का सम्बन्ध बना, ये सभी चीज़ें शिक्षा की प्रकृति में शामिल हैं। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति गाँव में रहते हुए शिक्षित हो जाता है, वो गाँव में रहने में अटपटा महसूस करने लगता है। इस मानसिक स्थिति में आप उन तमाम तत्वों को ढूँढ़ सकते हैं जो शिक्षित व्यक्ति एवं अन्य अशिक्षित या असाक्षर ग्रामीणों के सम्बन्धों को प्रभावित करते हैं। उसमें एक सोच विकसित हो जाती है कि मैं शिक्षित हूँ, अन्य ग्रामीणों से ऊपर उठ गया हूँ, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता या मेरी तकदीर अब मुझे कहीं और ले जाएगी। यहाँ शिक्षा एक काफी बड़ा हस्तक्षेप उसकी आत्मछवि में और अपने गन्तव्य में करती है। इसका आशय यह है कि शिक्षा के ज़रिए वो स्वयं को शेष से बेहतर समझने लगता है। जहाँ ‘बेहतर’ का अर्थ ज्ञान और संस्कृति से सम्बन्धित तो है ही, साथ ही शिक्षित व्यक्ति एक ‘नैतिक श्रेष्ठता’ का दावा भी करने लगता है। वह समझता है कि अब वह शिक्षा से जीवन का एक बेहतर उद्देश्य प्राप्त करेगा जबकि अन्य व्यक्ति इस बात में कच्चे हैं। इस तरह शिक्षा एक प्रकार की अहमन्यता को जन्म देती है, जो सीधे-सीधे उस शिक्षित ग्रामीण व्यक्ति को गाँव से असन्तुष्ट बनाती है और उसे गाँव से तोड़ती है।
प्रश्न - शिक्षा से जुड़ी इस ‘नैतिक श्रेष्ठता’ का इतिहास क्या रहा है और इसके प्रभाव की थोड़ी विस्तार में चर्चा करें।
इसके उत्तर के लिए हमें औपनिवेशिक समाज पर कुछ चर्चा करने की ज़रूरत है। औपनिवेशिक समाज ने भारत में आधुनिक शासन व्यवस्था और आधुनिकता की तस्वीर रची और ये समाज इस मान्यता पर आधारित था कि हम जहाँ हैं... वहाँ रहना ठीक नहीं है। अगर हम किसी लायक हैं तो हम वहाँ से ऊपर उठेंगे या हटेंगे। इस सिलसिले में, गाँव में जो शिक्षित होगा वह शहर पहुँचेगा, जो शहर में शिक्षित होगा वह विदेश पहुँचेगा। इसमें औपनिवेशिक मानसिकता का यह सूत्र छिपा हुआ है कि ये औपनिवेशिक शक्तियाँ श्रेष्ठ हैं और इसी श्रेष्ठता के कारण वे शासन स्थापित करने में सफल रहे हैं। उस शासन की स्थापना में आपको ताकत व हथियार का प्रयोग मिलेगा, आपको अन्य परिस्थितियाँ (जिनका निर्माण औपनिवेशिक विजय में होता था) भी मिलेंगी। लेकिन इनको शिक्षा से अर्जित नैतिक श्रेष्ठता का दावा छिपा लेता था। इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक (जो कि औपनिवेशिकता के सन्दर्भ में लिखी गई है) में सिद्ध करने का प्रयास किया है कि औपनिवेशिक शासन केवल एक पद्धति नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है और विचारधारा का अर्थ ही ये होता है कि वो वास्तविक उद्देश्य को छिपाकर उसके ऊपर एक मुल्लमा लगा देती है। शिक्षा ने इस मुल्लमे को लगाने में बड़ी भूमिका निभाई है। शिक्षा के ज़रिए वो नैतिक श्रेष्ठता अर्जित होती है जिसमें अपनी परिस्थिति से हटना और किसी दूसरी परिस्थिति से जुड़ना, ये अनिवार्य रूप से निहित है। चूँकि गाँव वो एक अन्तिम इकाई है, जहाँ उसका प्रभाव धीरे-धीरे पहुँचता है और इस प्रक्रिया में गाँव की प्रतिभाओं एवं क्षमताओं को वहाँ से निकालना और अन्यत्र लगाना, दोनों ही शामिल हैं। यह शिक्षा का उद्देश्य पहले भी था और आज भी है।
आज भी देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पढ़-लिखकर गाँव से चला गया है, तो उसे यही कहकर याद किया जाता है कि बहुत ही सही निकले। ‘निकले’ का अर्थ ही है कि यहाँ से निकल गए, इस रूपक को आप साहित्य में ढूँढ़ सकते हैं। जैसे ‘रागदरबारी’ को देखें, तो इसमें जो मुख्य नायक है, एक गाँव से निकलकर जे.एन.यू. तक पहुँचा है और अब वह गाँव में छुट्टियाँ मनाने आया है। गाँव की उन छुट्टियों के दौरान उसे गाँव की राजनीति या उसकी तलछट से गुज़रने का मौका मिलता है, जिसके बाद वह फिर वापिस भागता है। अब उससे ज़्यादा समय वह वहाँ खर्च नहीं कर सकता क्योंकि उसका मन कहीं और जुड़ चुका है और गाँव रहकर वह इस संघर्ष से नहीं गुज़र सकता। यह एक वास्तविक स्थिति का या एक यथार्थ का चित्रण है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गाँव से उसकी क्षमताएँ, उसकी प्रतिभाएँ धीरे-धीरे छिनकर या कहें छनकर शहर पहुँचती हैं और शहर से महानगर और महानगर से विदेश। विदेश भी कौन-सा? जहाँ से औपनिवेशिक सम्बन्धों के सूत्र शुरु होते हैं। यह एक पूरा सिलसिला है, जिसमें शिक्षा ने बड़ी भूमिका निभाई है और आज भी निभा रही है।
प्रश्न - अगर मैं इस बात को ऐसे समझने का प्रयत्न करूँ कि औपनिवेशिक काल में जो सम्बन्ध एक अँग्रेज़ व्यक्ति का एक भारतीय व्यक्ति के साथ था, ऐसा ही कुछ सम्बन्ध आज शहर और गाँव के बीच बन चुका है तो मेरा ये मानना, कहाँ तक उचित है? इस सामाजिक परिवर्तन के शिक्षा के अलावा और कौन कारक रहे हैं या सिर्फ शिक्षा ही एक मुख्य कारक है?
जी हाँ, आप काफी निकट पहुँच गए हैं, इस बात के कि यह एक प्रकार का सम्बन्धशास्त्र है। इसकी जड़ में वही सम्बन्ध है कि शिक्षा पाकर एक व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ हो जाता है। लेकिन शिक्षा का यह रूप औपनिवेशिक प्रवृत्तियों के अलावा एक पुराने संस्कार को भी लिए हुए है। इस संस्कार को एक रूपक से समझा जा सकता है। यह रूपक स्कूलों में अक्सर प्रयोग में लाया जाता है कि शिक्षित व्यक्ति एक कमल के समान है जो कीचड़ से ऊपर उठ जाता है। इस रूपक में एक प्राचीन विचार निहित है कि जो व्यक्ति ज्ञान व विद्या की दृष्टि से स्थापित हो गया अर्थात् शिक्षा पा गया और जिसे उसने पीछे छोड़ दिया है, वो एक प्रकार का कीचड़ है। वह शिक्षित व्यक्ति बाकी लोगों से श्रेष्ठ है, इसलिए ऊपर खिल रहा है। यह एक प्राचीन विचार था जोकि औपनिवेशिक काल में एक नए रूप में दृढ़ हो गया।
जिसको आज की शब्दावली में मानव संसाधन कहते हैं, वास्तव में वो एक प्रकार का प्रतिभा का व्यापार है, प्रतिभा का निर्यात है जिसमें नीचे की इकाइयों से प्रतिभा को खींच-खींच कर निर्यात करने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में जो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए ये वंचित होने की बजाय गर्व का कारण बन जाता है। जैसे आप आज भी गाँव में जाएँ और पूछें कि “भई! यहाँ से कौन-से लोग पढ़-लिखकर निकले हैं?” तो आपको ये बात गर्व से बताई जाएगी कि जो फलाँ जज है, फलाँ ज़िले में या कोई डॉक्टर लगा हुआ है पास के शहर में, वो हमारे गाँव का लड़का था। इस पूरी मनोदशा में भी वो सम्बन्ध स्थापित हो जाता है कि हमारे जो श्रेष्ठतर हैं वो बाहर चले गए। इससे यह सिद्ध होता है कि यह एक प्रकार का सम्बन्धशास्त्र है, जिसमें जो निकला वह भी खुश और जिसने भेजा वह भी खुश। उनका गाँव से निकल जाना, आज गाँव को ऐसा कुछ महसूस नहीं कराता कि हमने अपने बेहतर युवक-युवतियों को खो दिया है। बजाय इसके, वे गर्व महसूस करते हैं। इस सम्बन्धशास्त्र का एक सामाजिक मनोविज्ञान है, जो शिक्षा में केन्द्रित है। यह शिक्षा के ज़रिए ही होता है कि हम सिद्ध करते हैं कि यह श्रेष्ठ है या सबसे अच्छा है और फिर उसे कहीं और इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जैसा कि आपने पूछा क्या ‘सिर्फ शिक्षा ही है’, तो ज़ाहिर है कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं है। इसमें अर्थव्यवस्था भी है, इसमें पूरी राजनीति भी है कि विकास कहाँ होगा। विकास यानी कि प्रकृति के संसाधनों का दोहन कहाँ से किया जाएगा और उनका निवेश कहाँ होगा। ग्रामीण परिवेश या वनों से प्राकृतिक संसाधन अगर निकलते हैैं, तो उनका निवेश शहरी केन्द्रों में या निर्यात के लिए अन्यत्र जाएगा। इस प्रकार यहाँ एक आर्थिक सम्बन्ध भी स्थापित हो जाएगा। जैसे मज़दूर गाँव से आएगा, फ्लाईओवर शहर में बनेगा। सामग्री गाँव से आएगी, उसका प्रयोग शहर में होगा। गाँव और शहर का सम्बन्ध जैसे सन्दर्भ में देखना चाहेंगे, उस सन्दर्भ में आपको एक समीकरण मिलेगा।
प्रश्न - यहाँ पर एक प्रश्न शिक्षा की भूमिका पर उठता है कि जो गाँव में पढ़ गए और फिर वे गाँव छोड़कर जा रहे थे, तो शिक्षा ने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो कुछ सोच क्यों नहीं पाए?
शिक्षा ने तो उन्हें जाने के लिए तैयार किया है क्योंकि शिक्षा ने व्यक्ति में एक नैतिक श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न किया। इसमें एक समस्या शिक्षा की विषयवस्तु की अवश्य ही ज़ाहिर होती है। अब हमें पहले यह सोचने की ज़रूरत है कि आखिर शिक्षा क्या है। शिक्षा एक तरफ चयन की एक प्रक्रिया है जो परीक्षा की धुरी के ज़रिए काम करती है। मतलब शिक्षा बहुतों में से कुछ को छाँटती है। इस प्रकार शिक्षा छाँटने की एक वैध विधि है और छँटे हुए पर मोहर लगाती है कि यह बाकियों से बेहतर है। शिक्षा का दूसरा काम इसकी विषयवस्तु पूरा करती है, गाँव और शहर में एक प्रकार के द्वैध (डुप्लीकेशन) को बनाकर। इसमें शिक्षा की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और इनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान में काम करने वाली वैचारिकी को शामिल किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर पिछले 150 वर्षों की पाठ्यचर्याओं या पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करें, तो आप पाएँगे कि हर एक विषय के ऊपर इस विचार की छाया है कि गाँव में रहने वाले लोग हर दृष्टि से अविकसित, लाचार या गँवार होते हैं। उनमें अन्धविश्वास या परम्पराओं की जकड़ अधिक होती है। जबकि शहरी लोगों में यह जकड़ कम हो जाती है और स्वास्थ्य या जागरूकता की दृष्टि से वे गाँव के लोगों के मुकाबले खुल जाते हैं या अधिक समझदार हो जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा की विषयवस्तु समझदारी और नासमझी का एक द्वैध गाँव और शहर के बीच बनाती है।
इस दौर की पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन के दौरान ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहाँ कहानियों, नागरिक शास्त्र और इतिहास की किताबों के माध्यम से यह बात सिखाई जाती है कि जो शिक्षित होकर शहर में रहने लगा है वह व्यक्ति अब जाति के बन्धनों, अन्धविश्वासों इत्यादि से मुक्त हो गया है। उसकी दृष्टि ज़्यादा जागरूक हो गई है या वह ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गया है। जबकि गाँव में एक विपरीत स्थिति का चित्रण किया जाता है। इन्हें गाँव के लिए स्टीरियोटाइप कहेंगे और ऐसे स्टीरियोटाइप आपको सीधे-सीधे व्यक्त होते हुए मिल जाएँगे। इनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। जाति गाँव में भी उतनी ही है, जितनी शहर में है। लेकिन शिक्षा पाकर हमारे दिमाग में ये स्टीरियोटाइप आ जाता है कि गाँव का व्यक्ति अधिक जातिवादी होता है और शहर में आकर उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब यह सवाल उठता है कि ये स्टीरियोटाइप कहाँ से आते हैं। ज़ाहिर है, यह सब शिक्षा की विषयवस्तु की देन है, समय से इसे चुनौती नहीं दी गई है इसीलिए यह बढ़ती जाती है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक इत्यादि में इस मानसिकता को रखने वालों का ही योगदान रहता है, इसलिए ये मानसिकता पीढ़ी-दर-पीढ़ी पुष्ट होती जाती है।
प्रश्न - आपने जो बात कही, जो उदाहरण दिए, उनसे मैं सहमत हूँ। बल्कि मैं इसमें कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा। यदि कोई व्यक्ति कोई पुरानी बात रख देता है या कुछ हटकर कह देता है तो उसे कुछ बातें सुनने को मिलती हैं जैसे “भैया! गाँव से आए हो क्या?” या “गाँव के रहने वाले हो क्या?” इसी से सम्बन्धित मेरा अगला प्रश्न है कि गाँव के लोगों को सीधा, सरल या परम्परावादी कहा जाता है और गाँव को पिछड़ा माना जाता है, जबकि शहर के लिए ये विचार एकदम उलट है। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं?
व्याकरण की दृष्टि से गाँव और शहर का एक युग्म बनता है। आप चौथी-पाँचवीं की कक्षा में आज भी बच्चे को विलोम पढ़ते हुए देखेंगे जहाँ गाँव का विलोम शहर बताया जाता है। यह एक प्रकार की धुव्रीकरण की मानसिकता है, इसको अगर गहराई से जाँचें जो अपने आप में एक गम्भीर प्रश्न है कि क्या वास्तव में गाँव शहर का उल्टा है? क्योंकि गाँव एक ऐसी इकाई है जिसको आप बुनियादी इकाई कह सकते हैं, बुनियादी इस अर्थ में कि वहाँ मनुष्य प्रकृति के साथ जूझ कर जीता है। अगर गाँव की एक ज्ञानमीमांसीय परिभाषा दी जाए तो गाँव को इस तरीके के युग्म में बाँधना उचित नहीं है, और न ही शहर को गाँव के युग्म में बाँधना उचित है। ये अस्तित्व के दो स्वरूप हैं। आप यह कह सकते हैं कि इनमें व्यापार के सम्बन्ध हो सकते हैं या अन्य प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं, लेकिन ये एक-दूसरे के विपरीत हैं यह मान्यता है। इस मान्यता के चलते हम उस विचारधारा में बह जाते हैं या फँस जाते हैं जिसमें हम मानने लगते हैं कि गाँव शहर से पिछड़ा हुआ है या इसमें जो श्रेष्ठतर तत्व था, वो शहर चला गया है। इस प्रकार हम गाँव और शहर में एक प्रकार से फर्क करने लगते हैं। जो आपने मुहावरा दिया वो भी इस बात को दर्शाता है, जैसे शहर में चार आदमी मिले तो वे एक-दूसरे से पूछते हैं कि ‘आप कहाँ के रहने वाले हैं’, जहाँ इसका मतलब यह है कि आप कौन-सी धरती छोड़कर यहाँ आए हैं? यानी शहर वो जगह है जहाँ हम कहीं से आते हैं और इसलिए आते हैं क्योंकि जहाँ से आए हैं वहाँ के बारे में हमारा भाव है कि वहाँ अब कुछ नहीं है। हमारे जैसे लोग वहाँ बसर नहीं कर सकते। इसके साथ ही एक भाव और भी है कि क्योंकि हम उस जगह को छोड़कर आए हैं इसलिए थोड़ा-सा कष्ट भी सहन कर रहे हैं। इसमें जो मातृ वाला रूप है वो भी कहीं-कहीं एक भावनात्मक गन्ध लिए हुए जीवित रहता है। मतलब इसमें एक प्रकार की नैतिक श्रेष्ठता भी शामिल है कि हम वे लोग हैं, जिन्हें ये कष्ट गँवारा हुआ और जो नहीं सह सके वे अभी भी वहीं फँसे हुए हैं।
साहित्य में भी यह बात काफी पुष्ट होती है कि किस प्रकार एक व्यक्ति एक जगह से उखड़कर हट जाता है और फिर प्रगति का प्रतीक बन जाता है। आधुनिकता की दृष्टि में, आधुनिकता की अवधारणा के निर्माण में प्रगति का रूपक गाँव छोड़ने में निहित है। गाँव के टूटने, बिखरने या घटने में देश की प्रगति का जो संकेत है, ये पूरा प्रतीक जगत इसी तरह बना है। इतना ही नहीं, आधुनिक समय में आधुनिकता के सन्दर्भ में किसी देश की प्रगति की माप उसमें ग्रामीण प्रतिशत के आधार पर की जाती है। अगर आप यूरोप को देखें तो आपको बताया जाएगा कि यहाँ ग्रामीण जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 3 या 5 प्रतिशत है और भारत में अभी भी 60 प्रतिशत से ऊपर लोग गाँव में हैं। इससे पता चलता है कि यूरोप के देश भारत से अधिक विकसित हैं और भारत अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। ये एक प्रकार की ज्ञानमीमांसा है, इसमें व्यक्ति, देश, दुनिया सभी को रखकर आप आधुनिकता को औपनिवेशिकता की देन के रूप में समझ सकते हैं।
शिक्षा, इसका एक विराट साधन है, जो हमारे दिमाग में गाँव को लेकर हीनता बोध और शहर को लेकर एक उपलब्धि बोध रचती है। अगर कोई पढ़-लिखकर गाँव नहीं छोड़ पाता, तो उसके प्रति एक लाचारी या अन्याय का भाव आता है कि ये पढ़-लिखकर भी खेती ही कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है। इस प्रकार गाँव के साथ ये जो एक संस्कार जुड़ा हुआ है, उसके कई रूप हैं। हालाँकि, आप देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में काफी पहले ही ये समझ लिया गया था कि जो भी शिक्षित हो जाएगा, वो ज़मीन से निश्चित रूप से हट जाएगा। उसकी अस्मिता ही उसे गँवारा नहीं करेगी कि अब वह यह सब काम करे। यह उसके लिए स्वाभाविक मान लिया जाता है कि वह कुर्सी पर बैठकर कोई काम करे, कोई शारीरिक काम उसके लिए उचित नहीं है। शिक्षा के साथ ये जितने संस्कार जुड़े हुए हैं, ये औपनिवेशिक आधुनिकता की रचना करते हैं।
प्रश्न - एक व्यक्ति जो गाँव छोड़कर शहर पहुँचा है, शहर उसे किस प्रकार स्वीकार करता है? क्या ये सम्भव है कि वह व्यक्ति अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि या मानसिकता से पूर्णरूप से मुक्त हो सकता है?
यह मुक्त होने का प्रश्न काफी जटिल है और ये एक विचार की माँग करता है कि आखिर वह व्यक्ति किस चीज़ से मुक्त हो रहा है। गाँव और शहर केवल दो भौगोलिक स्थितियाँ हैं लेकिन इन स्थितियों में एक से दूसरी जगह जाने में कुछ मान्यताएँ और प्रवृत्तियाँ काम करती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये जो दिमाग का ढाँचा है क्या वह बदल सकता है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें भारतीय समाज की मूल संस्थाओं की ओर जाना होगा जैसे जाति, एक मूल व बुनियादी संस्था है जिसके ज़रिए विवाह, श्रम, सम्बन्ध आदि चीज़ें संचालित होती हैं। जाति जन्म के आधार पर समुदाय और अस्मिता की रचना करती है, जिसमें मानसिक ढाँचा जाति की व्यवस्था के ज़रिए काम करता है। सिर्फ इस बात से कि आप गाँव से शहर में आ गए, क्या इस मानसिकता से मुक्ति पाई जा सकती है? अगर ऐसा होता तो जाति का दबदबा शहर के समाज में नहीं दिखता या शहरों में होने वाली शादियों या अन्य अनुष्ठानों में जाति का प्रभाव न दिखता। अगर ये मानसिकता बदलती, तो शहरों में स्वर्ण और निचली जातियों का यह सम्बन्ध न बना रहता। इस बात के शहरों में स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि शहरों में जाति के आधार पर उद्यम तय होते हैं। अगर ढूँढ़ने की कोशिश करें तो आप पाएँगे कि शहरों में सफाई कर्मचारी किसी निचली जाति के होते हैं, उसमें स्वर्ण जाति के लोग मिल पाना कठिन है और इसका उल्टा भी देखें तो हमें मिलता है कि ढाबे और रेस्तराँ में खाना बनाने वाले स्वर्ण जाति के होते हैं, उसमें कोई निचली जाति का व्यक्ति नहीं मिलता। मसला बस यह नहीं है कि जब गाँव के स्कूल में मिड-डे मील बँटता है और उच्च जातियों के बच्चे उसे खाने से हिचकिचाते हैं और इस आधार पर हम कह देते हैं कि गाँव में ही जाति व्यवस्था चलती है। यही व्यवस्था शहरों में भी चलती है। लेकिन वह हमें दिख नहीं पाती क्योंकि शहरों का स्टीरियोटाइप हमारे दिमाग पर इतना हावी होता है कि हम सोच नहीं पाते। हम स्टीरियोटाइप की एक ाृंखला में स्वंय को बाँध लेते हैं।
प्रश्न - आजकल सरकारी नीतियों या दस्तावेज़ों में दो शब्द ‘आदर्श गाँव’ और ‘स्मार्ट सिटी’ बहुत प्रचलित हैं। इन शब्दावलियों से गाँव और शहर के कौन-से लक्षण स्पष्ट होते हैं?
आपने यह बहुत अच्छा सवाल उठाया। इस सवाल के उत्तर में हमें एक कदम पीछे जाना पड़ेगा कि गाँव का विकास या ग्रामीण विकास जो कि एक सरकारी मुहावरा बन चुका है जो आज से नहीं लगभग सौ वर्ष पहले अँग्रेज़ों के शासनकाल से ही शु डिग्री हो चुका था। जब हम उस गाँव को खोजते हैं जिसका विकास हो रहा है या हो चुका है, तो हम पाएँगे कि ये वे गाँव हैं जो शहर से जुड़ रहे हैं। ये गाँव, गाँव की दुर्गमता या स्टीरियोटाइप से ऊपर उठ रहे होते हैं। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि गाँव और शहर हमारे मन में लक्षणों के ज़रिए बना हुआ एक युग्म है और जहाँ ये शहर जैसे लक्षण नहीं हैं, वो जगह गाँव है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे सड़क। सड़क मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि सड़क शहर में पाई जाती है और जहाँ ये सड़क नहीं है, वो गाँव है। जिस दिन गाँव में वो सड़क बन जाएगी तो उस दिन वह गाँव विकसित कहलाएगा। यह बात हरेक चीज़ पर लागू होती है, इसलिए गाँव के सारे विकास के पीछे ये दृष्टि काम करती है।
शिक्षा की दृष्टि से देखें, जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा गाँव की प्रतिभा को शहर ले जाती है, आपको बहुत-से ऐसे गाँव मिलेंगे जहाँ अब केवल पिछली पीढ़ी रह गई है क्योंकि युवा वर्ग या उनके बच्चे अब शहरों में रहने लगे हैं। यह भी सही है कि उन्होंने अपने गाँव में पक्के मकान बनवा दिए हैं लेकिन उन गाँवों में जीवन नहीं बचा है। अब वो या तो शहर में शामिल हो जाएगा या वहाँ कोई सम्भावना नहीं बचेगी कि वे गाँव का प्रतीक बन सकें। आदर्श गाँव वह गाँव होगा जो शहर जैसा दिखता होगा या जो शहर के लक्षणों से मेल खाता होगा, जबकि ये आदर्श गाँव या शहर के लक्षण नहीं हैं। बल्कि ये लक्षण मनुष्य के लिए एक आवश्यकता है।
जहाँ तक आपने स्मार्ट सिटी का सवाल उठाया है, यह इस समय की उत्तर-आधुनिकता से उपजा हुआ जुमला है कि शहर का विकास तब अपने पूर्णरूप में माना जाएगा, जब वो स्मार्ट बन चुका होगा। स्मार्ट का यह मुद्दा पश्चिमी राष्ट्रों की संस्थाओं की देन है। आप इसे उन स्कूलों से जोड़कर समझ सकते हैं, जो स्वयं को क्ष्च्ग्र् से प्रमाणित बताते हैं। जिन्हें यह प्रमाणपत्र किन्हीं खास ज़रूरतों को पूरा करने के आधार पर दिया जाता है। इस उत्तर औपनिवेशिक युग में औपनिवेशिकता एक राजनीतिक अर्थ में नहीं है, परन्तु मानकों का रचा जाना इस बात को सिद्ध करता है कि औपनिवेशिकता आर्थिक रूप में आज भी जीवित है। ये मानक वहीं रचे जाते हैं, जहाँ पर औपनिवेशिक शक्ति प्रस्फुटित हुई थी, इसमें अन्तर सिर्फ यही है कि यह अब यूरोप तक ही सीमित नहीं है, इसमें अमेरिका भी शामिल हो चुका है। ये राष्ट्र निश्चित करते हैं कि क्ष्च्ग्र् की यह मोहर हम किसे दें। जिसे पाने के लिए बाकी सभी राष्ट्र लालायित हो उठते हैं।
ये ‘स्मार्ट’ शब्द हमें उस औपनिवेशिक परम्परा का ध्यान दिलाता है जिसके अनुसार मानकों को रचना उनका काम है और मानकों के लिए जद्दोजेहद करना हमारा काम है। इसे एक रूपक के द्वारा समझा जा सकता है। विनोद कुमार शुक्ल की रचना ‘नौकर की कमीज़’ जिसमें मालिक ने एक कमीज़ सिलवा ली है और अब जो भी नौकर बनेगा, उसे वह कमीज़ पहननी पड़ेगी। इसीलिए वह मालिक, नौकर इसी आधार पर चुनता है कि जो इस कमीज़ के आकार में फिट हो जाए, वह नौकरी के काबिल समझा जाता है। इस रूपक के आधार पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी साँचा और आदर्श कोई और तय करेगा, जिनमें हमें फिट होकर दिखाना है। तो यह नौकर की कमीज़ है जिसके लिए शिक्षा हमें तैयार करती है और उस कमीज़ को पहनने के बाद हम नौकर कहलाने के लायक हो जाएँगे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि औपनिवेशिकता किसी एक देश या दूसरे देश की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक वैश्विक प्रक्रिया है जिसने इस आधुनिक दुनिया का निर्माण किया है। इस विश्व रचना को ध्यान में रखते हुए अगर हम भारतीय गाँव को समझने का प्रयत्न करें तो उसकी लाचारी और उसपर ढहते कहर हमारी समझ में आ सकते हैं।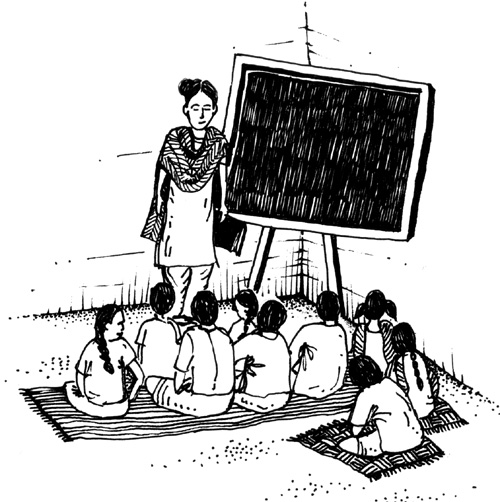 प्रश्न - शिक्षा की दृष्टि में गाँव की छवि किस प्रकार बनती है? औपनिवेशिक शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा और आज की शिक्षा के दृष्टिकोण में किस प्रकार का परिवर्तन आया है?
प्रश्न - शिक्षा की दृष्टि में गाँव की छवि किस प्रकार बनती है? औपनिवेशिक शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा और आज की शिक्षा के दृष्टिकोण में किस प्रकार का परिवर्तन आया है?
औपनिवेशिक शिक्षा और उसके बाद शिक्षा में जो प्रवृत्तियाँ चली आ रही हैं, उनमें शिक्षित होने का मतलब गाँव को परम्पराओं का शिकार समझना या गाँव को हेय दृष्टि से देखना है। यह शिक्षा यही सिखाती है कि गाँव पिछड़ेपन का प्रतीक है। असल में शिक्षा पाने की प्रक्रिया ही ऐसी है जो गाँव से निकलने की माँग करती है। पहले के समय में गाँव में स्कूल नहीं थे। अब गाँव में स्कूल तो हैं लेकिन थोड़ा भी आगे पढ़ने के लिए गाँव छोड़ना पड़ता है। ऐसा ही कुछ ज़िक्र एक अफ्रीकी लेखक ‘कमारा लये’ ने अपनी रचनाओं में किया है कि गाँव को छोड़े बगैर आदमी शिक्षित नहीं हो सकता। गाँव में आप एक सीमा तक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अगर उससे आगे आपको जाना है तो आपको स्कूल छोड़ना पड़ेगा। यहाँ एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि अगर आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर जाना पड़ेगा। यदि आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप गाँव में रहकर खेतों में या किसी दुकान पर ही काम करेंगे।
औपनिवेशिक काल में शिक्षा और रोज़गार का वितरण बहुत मज़बूत हो चुका था, उससे जुड़ी प्रक्रियाएँ आज भी जारी हैं। दूसरी ओर पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तक और शिक्षक की अपनी दृष्टि गाँव को पिछड़ा बताने में काफी योगदान करती हैं। यहाँ पर अपना एक निजी अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जब 2005 में ग़्क्कङच्र् में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का निर्माणकार्य शु डिग्री हुआ, उसकी स्टीयरिंग कमिटी की अध्यक्षता प्रो. यशपाल कर रहे थे। उसकी पहली मीटिंग में ही आचार्य राममूर्ति (सदस्य) ने यह बात कही थी कि गाँव की छवि शिक्षा में अत्यन्त दुर्भावनापूर्ण है और अगर हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बना रहे हैं तो उसका उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब वह गाँव की छवि को निष्पक्ष ढंग से पेश कर सके। उनकी यह बात काफी वज़नी थी और बहुत सदस्य इस बात से सहमत थे, जिनमें अनिल सदगोपाल, अशोक वाजपेयी आदि शामिल थे।
पाठ्यचर्या की मंज़ूरी के बाद और पाठ्यपुस्तकों के बनने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखा गया कि पाठ और विषय चुनते समय गाँव को एक इकाई के रूप में पेश किया जाए, न कि पिछड़ेपन के संकेत के रूप में। यह एक बड़ी कोशिश थी, ऐसा भी नहीं है कि यह सौ प्रतिशत सफल रही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ‘पानी’, पानी को लेकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पुस्तक में एक पूरा अध्याय है, जिसमें एक गाँव में पानी एक केन्द्रिय विषय बनता है। शहर में पानी कहाँ से पहुँचता है, खेतों में पानी कहाँ से आता है -- इस पूरी प्रक्रिया को एक किसान के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। इसी तरह कानूनों को या जायदाद को एक किसान औरत के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश की गई है। अगर आप पाठ्यचर्या का अध्ययन जेंडर, विकास या प्रगति के दृष्टिकोण से करें तो आप पाएँगे कि खासकर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की पुस्तकों में ग्रामीण समस्याओं को केन्द्र बनाया गया है। इसमें गाँव की छवि को एक निरपेक्ष ढंग से और गाँव को समाज के एक बड़े हिस्से के रूप में पेश किया गया है। अन्धविश्वास जितना गाँव में है, उतना ही शहर में भी है या अगर हमें कोई राजनीतिक अध्ययन करना है, तो हम यह बिलकुल नहीं कह सकते कि गाँव का व्यक्ति जातिवादी ढंग से वोट देता है और शहरी व्यक्ति व्यक्तिगत चिन्तन के आधार पर वोट देता है। यह किसी सर्वेक्षण से भी सिद्ध नहीं होता है।
नौवीं-दसवीं की लोकतंत्र की किताब में पूरा ध्यान रखा गया है कि गाँव का स्टीरियोटाइप स्त्रियों, आदमियों या आदिवासियों का न बने, जिन्हें औपनिवेशिक काल और आज़ादी के बाद की पाठ्यपुस्तकों में केवल पिछड़ेपन के रूप में दर्शाया गया है। यह कोशिश एन.सी.ई.आर.टी. अपने उस समय के रुतबे और स्वायतता के कारण कर सकी परन्तु राज्यों की पाठ्यपुस्तकें अभी भी नहीं बदली हैं। अलग-अलग राज्यों की किताबों में गाँव के मकान को अभी भी पिछड़ेपन का और शहर के मकान एवं उसके बाहर खड़ी कार को अगड़ेपन का प्रतीक माना जा रहा है। इसमें हमने दो बातें कीं, एक शिक्षा की संरचना की और दूसरी शिक्षा की विषयवस्तु की। दोनों ही, उस यथार्थ की विविधता और उसकी गहराइयों को एक सपाट दृष्टि में गठरी बाँध कर पेश करते हैं। शहर को महत्व देने के साथ-साथ यह मान लिया गया है कि गाँव से आने वाली गाड़ी से आने वाले इसी शहर में समाँ जाएँगे। शिक्षा इसमें एक अहम भूमिका निभाती है।
प्रश्न - गाँव, अवसरों की कमी से किस प्रकार जूझ रहा है? शिक्षा जगत के कुछ उदाहरण लेकर अगर आप इसे स्पष्ट कर सकें।
गाँव शिक्षा की दृष्टि से, रख-रखाव की दृष्टि से, पानी या बिजली की हर प्रकार की दृष्टि से उपेक्षित रहा है। इस बात की पुष्टि सरकारी आँकड़े भी करते हैं और बताते हैं कि सभी बुनियादी ज़रूरतें गाँव के स्तर पर आकर लड़खड़ाने लगती हैं। अगर आप किसी आयोग का विश्लेषण करें तो आप पाएँगे कि 1200 पन्नों की रिपोर्ट में गाँव का ज़िक्र केवल दो या तीन बार होता है और वो किसी निश्चित सन्दर्भ में ही होता है जैसे गरीब लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति, कृषि की शिक्षा आदि। लेकिन कहीं भी गाँव को एक समाज के रूप में जगह नहीं मिली है। आपको यह हालात हर स्तर पर मिल सकते हैं जैसे योजनाओं के निर्माण, बिजली की उपलब्धता, स्वास्थ्य, मकान की उपलब्धता या बहुत ही नीचे की बुनियादी ज़रूरत का मुद्दा भी जाँच सकते हैं। जैसे शिक्षक की नियुक्ति, यह नियुक्ति शिक्षक के लिए एक मकान की माँग करती है। जबकि पिछले कुछ 30 वर्षों में महिलाओं की बतौर शिक्षिका नियुक्ति बड़े पैमाने पर हुई है। इसी उदाहरण का अगर आप विश्लेषण करें तो आप पाएँगे कि एक महिला शिक्षिका किसी कस्बे या शहर से बस में गाँव के स्कूल में पहुँचती है। जहाँ स्कूल आठ बजे खुलता है, वह शिक्षिका बसों के कारण साढ़े आठ या नौ बजे स्कूल पहुँचती है। लौटते समय उस बस का समय अगर 12 बजे का है, जबकि स्कूल दो बजे तक चलता है, तो इसमें कोई हैरानी नहीं अगर वह शिक्षिका 12 बजे वापिस लौट जाती है। अगर सरकार ने स्कूल के साथ कोई क्वार्टर की योजना नहीं बनाई है तो यह ग्रामीण शिक्षा को काफी प्रभावित करने का कारण बन सकता है। शिक्षा के दस्तावेज़ों में अगर आप ढूँढ़ें तो आपको 1956 में ऐसी आखिरी रिपोर्ट मिलेगी जो शिक्षक की नियुक्ति के साथ मकान की बात करती है।
दूसरे उदाहरण के तौर पर अगर चुनाव के समय गाँव का अध्ययन करें तो आप पाएँगे कि स्थाई शिक्षकों या शिक्षिकाओं को ट्रेनिंग से वोट की गिनती तक कम-से-कम 15-20 कार्यकारी दिनों के लिए स्कूल से अलग रहना पड़ता है। यह सारा काम करने के बाद वे अपने बच्चों को उपलब्ध हो पाते हैं। यह स्थिति और विकट हो जाती है अगर चुनाव परीक्षा के दिनों में होते हैं। यह काफी सूक्ष्म स्तर के मुद्दे हैं जिनका कभी बड़े स्तर की योजनाओं में ज़िक्र तक नहीं होता। यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि गाँव नियोजन के परिदृश्य में हाशिए पर है। अगर यह कहा जाता है कि गाँव में पढ़ाई नहीं होती तो कोई बड़ी हैरानी नहीं है। सवाल यह है कि वहाँ आपने कौन-सी अच्छी योजना बनाई है। आशय यह है कि गाँव में लगातार अवसरों की कमी रही है। यहाँ अवसरों का मतलब यह है कि अगर मेरा जन्म गाँव में हुआ है, तो मुझे वहाँ रहते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास और उनको अभिव्यक्त करना मेरे लिए सम्भव होना चाहिए। लेकिन अभी अवसरों का मतलब बन चुका है कि रोज़गार मिल जाए, जबकि यह केवल अवसर का परिणाम है। आपने ऐसी व्यवस्था ही नहीं की जिनसे वहाँ का बच्चा अपनी क्षमता को विकसित कर सके और बड़ा होने पर उसे बताया जाता है कि वह उस लायक ही नहीं है। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसा कि इरावती कर्वे ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि गाँव एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ गाँव खेती पर निर्भर हैं तो कुछ जंगलों पर निर्भर हैं। किसी गाँव में तालाब है तो किसी में नहीं है। हर गाँव में एक किलोमीटर का रास्ता एक समान नहीं होता, आपको जाँचना होगा कि वह गाँव पहाड़ों में है या रेगिस्तान में या किसी तटीय क्षेत्र में। आप विभिन्न गाँवों के लिए एक समान योजना नहीं बना सकते। अगर एक लड़की जलाऊ लकड़ी लेने के लिए या पानी लेने के लिए जंगल में जाती है या दूसरे गाँव में जाती है तो आप कैसे स्कूल के समय को तय करेंगे।
दूसरा मुद्दा यह है कि जैसा कि इरावती कर्वे ने बहुत पहले स्पष्ट कर दिया था कि गाँव एक प्रकार के नहीं हैं। कुछ गाँव खेती पर निर्भर हैं तो कुछ जंगलों पर निर्भर हैं। किसी गाँव में तालाब है तो किसी में नहीं है। हर गाँव में एक किलोमीटर का रास्ता एक समान नहीं होता, आपको जाँचना होगा कि वह गाँव पहाड़ों में है या रेगिस्तान में या किसी तटीय क्षेत्र में। आप विभिन्न गाँवों के लिए एक समान योजना नहीं बना सकते। अगर एक लड़की जलाऊ लकड़ी लेने के लिए या पानी लेने के लिए जंगल में जाती है या दूसरे गाँव में जाती है तो आप कैसे स्कूल के समय को तय करेंगे।
यह बात अँग्रेज़ों के समय में जानी जाती थी कि गाँव की व्यवस्था को आपको ऋतुओं, प्राकृतिक संसाधनों या उपलब्धता के आधार पर समायोजित करना होगा, तभी कोई स्कूल ठीक से चल सकता है। औपनिवेशिक काल से गाँव को उपेक्षा की दृष्टि से देखने की समस्या हमें कभी गाँव को वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं देखने देती। गाँव का अध्यापक, जूनियर डॉक्टर आदि इन्हीं दुविधा में ही जीते हैं और अवसर पाते ही गाँव से अपना तबादला करवा लेते हैं। यह एक प्रकार का दुष्चक्र है, जिसका पुनरुत्पादन होता रहता है। यह औपनिवेशिक काल से अब तक लगातार हो रहा है। इसमें कोई व्यवधान तब तक नहीं आ सकता, जब तक गाँव को केन्द्र नहीं बनाया जाता और इसके बिना योजनाएँ सफल नहीं हो सकतीं।
प्रश्न - आज के समय में गाँव और शिक्षा के सन्दर्भ में गाँधी को पढ़ना कितना प्रासंगिक है?
गाँधी के समाजदर्शन को पढ़ने से भारतीय समाज में गाँव के महत्व को समझा जा सकता है। हिन्द स्वराज और अपने कई वक्तव्यों में गाँधी के इस दृष्टिकोण का पता चलता है जो इस बात का पक्ष लेता है कि गाँव एक इकाई के रूप में भारत के लम्बे इतिहास में विशेष तरह की सक्रियता प्रदर्शित करता रहा है। हिन्द स्वराज में इस बात का हवाला है कि गाँव का सत्ता (राजा या ज़मींदार) से रिश्ता एक सौदे के समान है, जो तब तक कायम है, जब तक सत्ता गाँव पर अत्याचार नहीं करती। गाँधी ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जो गाँव के अघोषित असहयोग को स्पष्ट करते हैं। इनमें गाँधी ने गाँव की सक्रियता का सन्देश पाया कि गाँव सत्ता के साथ अहिंसक तरीकों से जूझने का आदि रहा है। इनमें एक प्रकार की नैतिकता, कुछ सिद्धान्तों के ढाँचों में रह कर काम करती है। यह नैतिकता भाषा, धर्म, दैनिक आचार और सबसे अधिक गाँव के इकाईपन से व्यक्त होती है। आज भी यह प्रश्न काफी महत्व रखता है कि गाँव किस प्रकार अपनी नैतिकता को व्यक्त करता है क्योंकि आज हम जिस गाँव की चर्चा करते हैं वह औपनिवेशिक युग से गुज़रा हुआ एक गाँव है, जिसमें गाँव या तो टूट गया है या शहर में समा गया है। मुझे लगता है कि जो कुछ गाँधी ने गाँव के प्रति महसूस किया था, उस सन्दर्भ में गाँव को समझने में हम असक्षम हैं। अर्थात् ऐतिहासिकता के दर्पण में गाँधी के दर्शन को देखना आज हमारे लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि न तो हमारे पास उस तरह का कोई अनुसन्धान है और न ही उस सोच का कोई दार्शनिक विश्लेषण हुआ है।
गाँधी के उस गाँवत्व को आज नहीं समझा जा सकता क्योंकि आज हम गाँव को केवल शहर के विलोम के रूप में ही देखते हैं। हम नहीं सोच पाते कि गाँव का जीवन कृषि, प्रकृति या दस्तकारी के सन्दर्भों में जिया जा सकता है। अभी हाल में मुझे दक्षिण भारत की एक पीएच.डी. के अध्ययन का अवसर मिला जिसमें गाँव में ज्ञान को खेती, भूगोल, मौसम, दस्तकारी आदि के सम्बन्ध में समझने की कोशिश की गई है। बड़ा ही रोचक शोध था वह जिसमें इस ज्ञान परम्परा को यूरोप के विश्वविद्यालय की ज्ञान परम्परा से तुलना करके देखा गया है।
गाँधी ने नई तालीम के माध्यम से भारतीय समाज की पुन: रचना की जो कल्पना की थी वह कितनी यथार्थवादी है। इसी से जुड़ा एक शोध हुआ है जिसमें यह समझने का प्रयत्न किया गया है कि गाँव के स्तर पर दस्तकारियों से जुड़े सम्बन्ध किस-किस प्रकार के ज्ञान को जीवित रखते हैं। उस शोध में यह दिखाया गया है कि जिसे हम कौशल समझते हैं, उसमें बहुत-सा ज्ञान कई स्तरों पर निहित है। यह ज्ञान किसी दस्तावेज़ीकरण या किताबों के माध्यम से जीवित नहीं रहता बल्कि सम्बन्धों के स्तर पर जीवित रहता है। तो दोनों शोधकार्य गाँधी के ज्ञान सम्बन्धी और समाज सम्बन्धी दर्शन को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं।
आज मैं यही कह सकता हूँ कि उस समझ के पर्याप्त साधन हमारे पास नहीं हैं परन्तु वह दर्शन अपने आप में इतना वज़नी है कि हम उसको दरकिनार या खारिज नहीं कर सकते। आने वाले समय में हम यह भी समझ सकेंगे कि हम जिस प्रतिरोध क्षमता की बात करते हैं वो क्षमता आज के गाँव में किस प्रकार मौजूद है। अभी हाल ही में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आधुनिक समाज विज्ञान के अनुसार तो आप उसे लाचारी का प्रतीक कह सकते हैं लेकिन गाँधी की विचारधारा के अनुसार इसे एक प्रकार का प्रतिरोध कहा जाएगा कि मैं ऐसे समाज में नहीं जीना चाहता। अनुसन्धान की दृष्टि से देखें तो इस घटना का न राजनैतिक विश्लेषण हुआ है और न ही मनोवैज्ञानिक, थोड़ा-बहुत अर्थशास्त्र के आधार पर विश्लेषण हुआ है। हमारे पास किसान के जीवन को समझने के लिए पर्याप्त मनोवैज्ञानिक अवधारणा या अनुसन्धान ही नहीं हैं। ऐसा ही कुछ गाँव के साथ है। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि एक औपनिवेशिक देश होने के कारण हमारा एक आधा-अधूरा शिक्षा जगत है जो बहुत सीमित साधनों और वैचारिक स्त्रोतों की मदद से चल रहा है। इस चर्चा में हमें अपने ज्ञान के अधूरेपन को स्वीकारना होगा और इसीलिए किसी सम्यक निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता। परन्तु उन प्रश्नों को जीवित रखने की आवश्यकता है, जिन प्रश्नों को सौ वर्ष पहले गाँधी ने हिन्द स्वराज में उठाया था।
प्रश्न - शहरीकरण के इस दौर में कई अन्तर्राष्ट्रीय या ग्लोबल कहे जाने वाले स्कूलों की बाढ़-सी आ गई है। आपके अनुसार वास्तव में एक अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल में क्या होना चाहिए?
इस तरह के नाम से प्रचलित स्कूल केवल व्यापारिक स्कूल हैं। ये स्कूल सिर्फ नाम का दोहन करके अधिक फीस लेना या एक पूरी रेज़िडेंशियल व्यवस्था चलाने का व्यवसाय करते हैं। भारत के नवधनिक वर्ग जिसमें गाँव का भी एक नवधनिक तबका है, खास कर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों के गाँव इस तबके में शामिल हैं। इस वर्ग को इन स्कूलों का नाम आकर्षित करता है क्योंकि ‘अन्तर्राष्ट्रीय’ या ‘ग्लोबल’ का अर्थ ही हमें पश्चिम के करीब ले जाता है। पश्चिम का भी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है जिसका आशय मुख्यत: अमेरिका या यूरोप है। इनके भौतिक प्रतीक चौड़ी-सपाट सड़कें, ज़मीन के नीचे से बिजली के तार या नॉएडा में बना फॉर्मूला नम्बर-1 कार रेस का स्टेडियम आदि विकास के प्रतीक बन चुके हैं।
आजकल कैशलेस इकॉनमी की बात हो रही है। यह पूरा एक प्रतीक जगत बन चुका है, जिसका विश्लेषण किया जाए तो हम पाएँगे कि जो नकल करने की प्रक्रिया 19वीं सदी में शु डिग्री हुई थी, वह सिलसिला आज भी जारी है। इसका उद्देश्य अपने देश को वैसा दिखाना है जैसा अमेरिका या ब्रिटेन दिखाई देता है। जिस तरह हम औपनिवेशिक काल में जीते थे, आज भी वैसे ही हैं। हमारी अपनी कल्पनाशक्ति समाप्त हो चुकी है और हम उन्हीं की कल्पना पर जीवित हैं। हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा अगर इस अन्तर्राष्ट्रीय स्कूल में पढ़ जाएगा तो वह इस ग्लोबल बाज़ार में खपने लायक आधा तो तैयार हो ही जाएगा। अगर आप इस बात को वैश्वीकरण के ज़रिए समझें, जिसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार है, फिर उसके भीतर एक राष्ट्रीय बाज़ार है और उसके भीतर कई स्थानीय बाज़ार हैं तो जितनी दूर तक हम अपने बच्चे को विक्षेपित कर सकते हैं, उसकी शिक्षा उतनी ही सफल होगी। ऐसे स्कूल किसी भी मायने में अन्तर्राष्ट्रीय नहीं कहे जा सकते। भारत में लगभग ऐसे 500 स्कूल हैं जो सही में अन्तर्राष्ट्रीय हैं। वे जिनेवा या ब्रिटेन की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनका पाठ्यक्रम अलग है, परीक्षा व मूल्यांकन के तरीके अलग हैं लेकिन जिन स्कूलों की बात आप कर रहे हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं है। ये बस शिक्षा की एक नई पैकेजिंग है जो बिक रही है। जो सही मायने में इंटरनेशनल स्कूल हैं उन्हें इन स्कूलों से अलग करके देखने की ज़रूरत है लेकिन सामान्य लोग इस अन्तर को नहीं समझ पाते।
प्रश्न - ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले बच्चों पर ऐसे स्कूलों के प्रभावों को आप किस प्रकार देखते हैं?
यह खुद आपने अपने शोध में पाया है कि शहर बनते गाँव में खुला हुआ ऐसा स्कूल जिस वर्ग को आकर्षित कर रहा है वह एक तरह की दुविधाओं में जीने के लिए ही तैयार हो रहा है। जिस पीढ़ी के बच्चों से आपने वार्तालाप किया, उनके लिए इस समस्या का समाधान होने में ही बहुत लम्बा समय लग जाएगा। वो भी तब सम्भव है, जब शिक्षा इस बदलाव का प्रयास करे। इस प्रकार के स्कूल ऐसा प्रयास नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कूल तो बच्चों को परीक्षा से गुज़ार कर बाज़ार में लाने के लिए ही तैयार कर रहे हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक दुविधाओं को लेकर ही वे बच्चे जी सकते हैं। उनकी सोच, दृष्टि उन मुद्दों पर वैसी ही रहेगी, जो न केवल पारम्परिक है बल्कि दकियानूसी भी है और दूसरी तरफ अपने गाँव में शॉपिंग मॉल, पिज़्ज़ा-बर्गर और अन्य सुविधाओं के लिए लालायित रहेंगे। यह मनोविज्ञान कोई ज़्यादा अनोखा भी नहीं है, आज भारत का बहुत बड़ा शिक्षित वर्ग है जो इस प्रकार से बँटे हुए दिमाग से जीता है। उसी वर्ग में इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे शामिल हो जाएँगे।
प्रश्न - अँग्रेज़ी के प्रचार-प्रसार के इस दौर में गाँव को किस प्रकार समझा जा सकता है?
अँग्रेज़ी का प्रश्न वहीं बना हुआ है, जहाँ वह पहले था। सबसे पहले अँग्रेज़ी हमारे मानस में हीनता का भाव उत्पन्न करती है। हम इस भाषा को अपने समाज में वर्गीय बँटवारे को महसूस करने और उस बँटवारे में अपनी कुछ बेहतर जगह बनाने के लिए एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अँग्रेज़ी भारत में हैसियत और ताकत की भाषा है। अँग्रेज़ी औपनिवेशिक शक्ति की भाषा है और आज की यह आधुनिक दुनिया इन्हीं औपनिवेशिक भाषाओं से बनी है। अगर आप अन्य औपनिवेशिक भाषाओं का विचार करेंगे, इन्हीं निष्कर्षों पर पहुँच जाएँगे। जैसे अफ्रीका में फ्रेंच, दक्षिण अमेरिका में स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेश, दक्षिण पूर्वी एशिया के डच, स्पेनिश या अँग्रेज़ उपनिवेश, इन सभी में आधुनिक दुनिया का जन्म हुआ है। जिन क्षेत्रों में इन शक्तियों ने शासन किया, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या को समाए हुए हैं, उस जनसंख्या में ये भाषाएँ निरन्तर हीनता का सिंचन करती हैं।
आज भारत में एक तबका आपको ऐसा मिलेगा जो 19वीं सदी से अँग्रेज़ी भाषा के सम्पर्क में है और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी मिलेगा, जहाँ गाँव में पहली पीढ़ी में इस भाषा का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों के बीच में आपको हर स्तर पर अँग्रेज़ी प्रयोग करने वाले परिवार मिल जाएँगे। जो वर्ग इस भाषा को एक लम्बे समय से प्रयोग में ला रहा है, वह एक अभिजन वर्ग है। इसके अलावा अँग्रेज़ी आज इंटरनेट की भाषा बन चुकी है। जितने भी ऐप हैं, उनकी शर्तें इसी भाषा में होती हैं। आप एक कोर्ट के निर्णय को देख लीजिए, वो आपको इसी भाषा में मिलेगा। आप कोई भी उदाहरण उठाकर देख लीजिए, हर जगह आपको यह भाषा जाननी आवश्यक बन जाती है।
गाँव में अँग्रेज़ी भाषा को आगे बढ़ने का साधन मान लिया जाता है, जहाँ आगे का मतलब है, बाज़ार की व्यवस्था में एक ज़्यादा बड़े बाज़ार में प्रवेश करना। अब वह बच्चा कितनी अँग्रेज़ी सीख सकेगा, जहाँ अध्यापक स्वयं इस भाषा का प्रयोग करने में असमर्थ है। यह एक प्रकार का शिकंजा है जिससे गाँवत्व कमज़ोर पड़ता जाएगा। लेकिन गाँधी के अनुसार समझने का प्रयास करें तो यह भी एक प्रतिरोध का विषय है जो किस रूप में इतिहास में अभिव्यक्ति पाएगा, कोई नहीं कह सकता। यह भी सत्य है कि हम इन लक्षणों को पहचान अवश्य सकते हैं।
कृष्ण कुमार: प्रसिद्ध शिक्षाविद् एवं लेखक। शिक्षा के मुद्दों पर सतत चिन्तन एवं लेखन। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा के प्रोफेसर और एन.सी.ई.आर.टी. के निदेशक रह चुके हैं। भारत और पाकिस्तान में शिक्षा पर उनकी दो पुस्तकें, मेरा देश तुम्हारा देश और शान्ति का समर चर्चित रही हैं। उनकी हाल की पुस्तकों में शिक्षा और ज्ञान, चूड़ी बाज़ार में लड़की और बच्चों के लिए पूड़ियों की गठरी शामिल हैं।
मनीष: केन्द्रिय शिक्षा संस्थान, दिल्ली से एम.फिल. कर रहे हैं।
सभी चित्र: अंकिता ठाकुर: राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद से ग्राफिक डिज़ाइन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। बाल साहित्य और चित्रों में दिलचस्पी रखती हैं।



