रश्मि पालीवाल
पर्यावरण और शिक्षा
शिक्षा पर सोच-विचार जहां कहीं भी शुरू होता है तो यह बात ज़रूर उठ जाती है कि शिक्षा पर्यावरण आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकें बनाने वाले लोग इस बात से बहुत जूझते हैं और कई बार तो अंधी गलियों में भी फंस जाते हैं।
आज से 14 साल पहले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने-पढ़ाने वाले हम कुछ लोग यह सोचने के लिए जुटे कि स्कूलों में समाज-विज्ञान कैसे पढ़ाना बेहतर होगा। बहुत-सी बातें सोची गईं। उन सब में एक बहुत प्रचलित मान्यता बार-बार उभरकर आती थी कि बच्चों को उनके परिवेश और पर्यावरण के आधार पर पढ़ाना चाहिए। बच्चों के परिवेश में क्या क्या चीजें हैं, और उनके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है - ये सब बातें खूब होती थीं। इन बातों के बीच एक जनाब ने अचानक एक अलग ही सुर छेड़ दिया। बोले, कि बच्चों में नए परिवेश की बातें जानने का भी जबरदस्त कौतूहल होता है - और हमें इस जिज्ञासा भाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण के आधार पर जरूर पढ़ाया जाए - पर भिन्न पर्यावरणों की बातें भी शामिल रखी जाएं... "मैं सोच नहीं सकता कि कोई बच्चा 11 से 14 वर्ष की उम्र पार कर जाए, सामाजिक-विज्ञान पढ़ जाए, और कभी इग्लू का नाम भी नहीं सुना हो उसने।'' शायद उन जनाब के घर में छोटे बच्चे रहे होंगे। हम बाकी लोगों को उनकी बात थोड़ी बेसुरी-सी लग रही थी, पर उसमें किसी सच्चे अनुभव का विश्वास था -- तो वो बात मन में कहीं खटकती रही सालों तक।
अपना गांव - अपनी तहसील ...
कुछ समय बाद हमने खुद स्कूलों में जा कर बच्चों से बातचीत करना शुरू किया। मुझे याद है कि छठी कक्षा के तख्ते पर बच्चों ने अपने गांव का नक्शा कितने मज़े से बना डाला था। एक एक जना आता जाता और एक एक चीज़ नक्शे में भरता जाता। बाकी सब बच्चे चील की निगाह से परखते रहते कि कोई चीज़ थोड़ी भी। इधर या उधरे तो नहीं बन गई। ये बच्चे पहली बार नक्शा बना रहे थे - पर कितना सहज था पूरा अभ्यास। क्योंकि पर्यावरण आधारित था... है। न?
 इसी तरह, एक दूसरे गांव में तहसील का नजूल नक्शा हमने स्कूल के बरामदे में फैलाया था। तीसरी से आठवीं तक के बच्चों की भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। अपना गांव, अपने मामा का गांव, और चाचा की ससुराल का गांव और फलानी सड़क तो फलाना नाला झट-झट पहचान बनती गई - अपनी जानकारी की कसौटी पर तुलती गई .. जब ज़रूरत लगी तो अपने-आप ही संकेतों की सूची भी देख ली, बूझ ली, उपयोग कर ली।
इसी तरह, एक दूसरे गांव में तहसील का नजूल नक्शा हमने स्कूल के बरामदे में फैलाया था। तीसरी से आठवीं तक के बच्चों की भीड़ उस पर टूट पड़ी थी। अपना गांव, अपने मामा का गांव, और चाचा की ससुराल का गांव और फलानी सड़क तो फलाना नाला झट-झट पहचान बनती गई - अपनी जानकारी की कसौटी पर तुलती गई .. जब ज़रूरत लगी तो अपने-आप ही संकेतों की सूची भी देख ली, बूझ ली, उपयोग कर ली।
फिर, एक बार की बात है। हमने बच्चों से उनके गांव की खेती पर चर्चा की। कौन-सी फसलें हैं - किस तरह की मिट्टी में कौन-सी फसल होती है ...किन औजारों का उपयोग होता है ... आदि । बताया बच्चों ने और खूब बताया। उसके बाद वे अपेक्षा करते रहे कि हम भी कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे या करेंगे। मुझे याद है कि हम एक असमंजस का अहसास अपने अन्दर पाते थे कि चर्चा को कहां ले जाएं? हमें तो यही लगा था कि बच्चों को अपने पर्यावरण के बारे में बहुत जानकारी है, उसकी समझ भी है, और उन्होंने कई निष्कर्ष भी निकालकर रखे हैं। बल्कि सीखना तो हमें है। फिर उन्हें हमारे साथ की इस पूरी कवायद से क्या मिल रहा है? हम जैसे अजनबियों से परिचय का कौतूहल व रोचकता - और हमारे आगे मुखरता और आत्म-विश्वास का भाव? क्या यही सब?
 दो-चार मुलाकातों के बाद इस सिलसिले का रंग फीका पड़ने लगा। बच्चों को हम कुछ नया सीखने को नहीं दे पा रहे थे। वे थोड़ा उकताने, थोड़ा खिसियाने लगे - और फिर हमसे कहते -“तुम तो कोई कहानी सुनाओ ना?"
दो-चार मुलाकातों के बाद इस सिलसिले का रंग फीका पड़ने लगा। बच्चों को हम कुछ नया सीखने को नहीं दे पा रहे थे। वे थोड़ा उकताने, थोड़ा खिसियाने लगे - और फिर हमसे कहते -“तुम तो कोई कहानी सुनाओ ना?"
उन्हीं दिनों एक बार बच्चों के परिवार का इतिहास पता कर के लिखने का अभ्यास भी करवाया था। इसके लिए कुछ रोचक डिज़ाइनें डाल कर पुस्तिका भी साइक्लोस्टाइल कर ली थी। पुस्तिका उन्हें रोचक लगी। पर जानकारी काफी कम पता लगाई गई बच्चे कहते, “हमें मालूम नहीं", "हमने दादाजी से (या पिताजी) से पूछा तो वे डांटने लगे कि क्या बेकार की बातें पूछ रहा है।''
हमारे सामने यह सवाल उठ रहा था कि पर्यावरण से शुरू तो कर लें, पर फिर जाएं कहां? दरअसल शिक्षण का उद्देश्य इतनी-सी बात से स्पष्ट नहीं होता। विचार इस सवाल पर होना होगा कि हम अपने परिवेश को जितना जानते और समझते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो यह कैसे किया जाए? अपने परिवेश के बारे में हमारी खुद की समझ में किस बात की कमी रहती है?
नए तरीके, जानने के...
अपने परिवेश को जानने और उसकी व्याख्या करने के कई तरीके हम लोगों के पास पहले से हैं।
जैसे किसी परिस्थिति की व्याख्या करने में, या किसी बात पर निर्णय लेने में हम उपमाओं व प्रतीकों का इस्तेमाल कर हैं। उदाहरणों के जरिए बात रखते हैं ... कहते हैं, जैसे वो ... वैसे ये .....। आमतौर पर लोग तालिका नहीं बनाते, नक्शे नहीं बनाते, ग्राफ, स्तंभालेख भी नहीं। दुनिया को जानने की ये अलग तरह की विधियां हैं। अगर ये उपयोगी हैं तो उन्हें सीखना महत्व रख सकता है। इन्हें सीखने के लिए अपने पर्यावरण के उदाहरणों को माध्यम बनाया जाए तो सीखना आसान, असरदार और रोचक होगा।
जैसे गांव का नक्शा बनाने में मज़ा आया था, वैसे ही गांव की जानकारी एक तालिका में भरने में भी मज़ा आएगा। एक नई विधि से खेलने का मज़ा। इसी तरह, जैसे तहसील का नक्शा पढ़ने में मज़ा आया था, वैसे ही अगर तहसील के अलग अलग गांवों की पैदावार की तालिका पेश की जाए, या पिछले 50 सालों में तहसील के गांवों की पैदावार का ग्राफ पेश किया जाए - तो भी उसे पढ़ने में मजा आएगा। अपनी जानकारी की पुष्टि होगी - और दी जा रही जानकारी की परख की जाएगी। कोई नई समझ या नए निष्कर्ष शायद निकलें; और शायद नहीं भी निकलें। पर एक नई ‘विधि' को इस्तेमाल करने का परिचय मिल जाएगा।
संभव हैं नए रास्ते भी...
अपने पर्यावरण के अध्ययन से विकास के रास्ते समझने की कोशिश भी की जा सकती है।
उत्तराखण्ड पर्यावरण शिक्षा केन्द्र* की कार्यपुस्तकें एक ऐसे ही प्रयास की तरफ बढ़ती हैं। वे बच्चों को नक्शों, तालिकाओं, मापन अभ्यासों, स्तंभालेखों आदि के ज़रिए अलमोड़ा
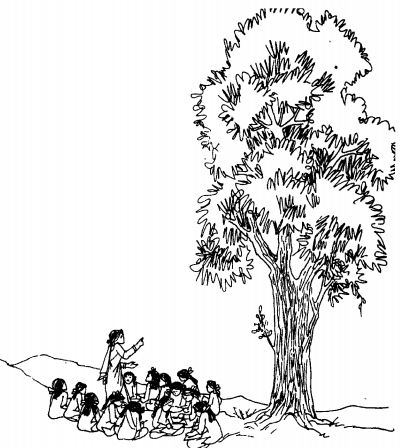 ‘उत्तराखण्ड पर्यावरण शिक्षा केन्द्र' द्वारा कक्षा-6 के लिए तैयार किताब 'हमारी धरती हमारा जीवन' के पाठ 'हमारे ग्राम वृक्ष' से लिया गया एक चित्र।
‘उत्तराखण्ड पर्यावरण शिक्षा केन्द्र' द्वारा कक्षा-6 के लिए तैयार किताब 'हमारी धरती हमारा जीवन' के पाठ 'हमारे ग्राम वृक्ष' से लिया गया एक चित्र।
क्षेत्र की वर्षा, नदी के बहाव, जमीन पर उगने वाले चारे की मात्रा आदि का लेखा जोखा करना सिखाती हैं। वे यह भी सिखाने की कोशिश करती हैं। कि अलमोड़ा क्षेत्र की धरती की उत्पादकता अभी की तुलना में कैसे बढ़ाई जा सकती है। यानी अपने पर्यावरण के बारे में वहां के बच्चे अभी तक जिस स्तर पर जानते और सोचते हैं, उस स्तर को आगे ले जाने की कोशिश ये किताबें करती हैं। पर्यावरण के विकास की एक खास तरह की योजना बच्चों के सामने रखती हैं। इस संबंध में, सोचने और जानने के लिए कई बाते हैं, जैसे, सुझाई गई योजनाएं कितनी उपयुक्त हैं, बच्चों से जो प्रायोगिक कार्य अपेक्षित है वो कितना व्यावहारिक और प्रभावी है, स्कूलों में बच्चे व शिक्षक इस तरह के पाठों को कितनी रुचि और गंभीरता से लेते हैं - ऐसी कई जिज्ञासाएं अपनी जगह हैं, तो भी इन पुस्तकों में ‘पर्यावरण' से शुरू करके जाएं कहां?' - इसका एक हल सामने आता है।
नए अनुभव कैसे जोड़ लेते हैं? ...
पर पर्यावरण के आधार पर और भी मंज़िलों पे पहुंचा जा सकता है।
अपने निजी जीवन का उदाहरण लें। हम औरों के किस्से, कहानियां उपन्यास ... टी. वी. सीरियलों .. से जुड़ाव महसूस करते हैं। दूसरों के अनुभव हमारी अपनी किसी कमी को पूरा करते हैं। हमारे अनुभवों का दायरा फैलाते हैं - तुलना करने और सोचने का नया साधन देते हैं। परी कथाएं हों या पौराणिक कथाएं - इनके कई पहलू तो हमारे पर्यावरण में मौजूद ही नहीं हैं -- न उड़न खटोले हैं, न अवतार हैं, न देवी दर्शन हैं। पर फिर भी इन कथाओं के कथानकों से हम कुछ सोच, कुछ समझ हासिल कर लेते हैं। कथाओं के मूल कथानक से जुड़ना संभव हो पाता है, इसलिए कथा की छोटी-छोटी अजनबी बातें कोई अड़चन नहीं बनतीं।
इस चीज़ को समझने और देखने का मौका पिछले दस सालों में कई बार मिला है। जिस ग्रामीण स्कूल के छात्रों के साथ हम उनके यहां की खेती-बाड़ी की चर्चा के बाद असमंजस में खड़े हुए थे - कि अब इस बात को कहां ले जाएं? उसी स्कूल के छात्रों के साथ हमने मुगल काल के गांवों व किसानों के पाठ के सन्दर्भ में बेहद जीवन्त चर्चाएं की हैं - जिसमें मुगल काल की परिस्थिति की भी विवेचना हुई और उसी की तुलना में आज के किसानों की परिस्थिति की भी हुई। एकदम सहजता से हुई, रोचकता से हुई। तो
इस जीवन्त बातचीत का कथानक क्या था? यह, कि जब किसान शासन के करों के दबाव से परेशान हों तो उनके सामने क्या विकल्प होते हैं, वे क्या कर सकते हैं? तब क्या करते थे? अब क्या करते हैं? क्यों? क्या बदला है?
इस सबसे बच्चों ने अपने परिवेश के बारे में क्या कोई नई या बढ़ी हुई समझ पाई? शायद हां। अपनी खुद की परिस्थितियों के बारे में सोचने विचारने के हमारे कुछ तौर तरीके बन गए होते हैं - जो कुछ हद तक हमें दूसरों से मिली नसीहतों का नतीजा भी होते हैं। मसलन हम कभी सोचते हैं - आज हालात इतने बुरे हैं कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता ... या हम सोचते हैं कि लोगों के दिल बुरे हो गए हैं इसलिए आज यह हाल है। पर जब हम मुगल काल के
 मुगलकाल के गांव का एक चित्र। यह चित्र अकबर के समय में बनाया गया था।
मुगलकाल के गांव का एक चित्र। यह चित्र अकबर के समय में बनाया गया था।
किसानों की जानकारी हासिल करते हैं ... तो शायद यह सोच भी उभर आए कि हालात तो तब भी अपनी तरह से बुरे थे - पर उस परिस्थिति में लोगों के सामने एक तरह का विकल्प था। आज की परिस्थिति में क्या विकल्प है?
बच्चे इस बात पर बहुत हंसे थे कि मुगलकाल में किसान अगर अपनी ज़मीन छोड़ कर चले जाएं और कुछ साल बाद लौटें तो उन्हें उनकी ज़मीन जोतने के लिए फिर से मिल जाती थी। बोले ‘‘आज तो कोई न छोड़े .. . और छोड़े तो दूसरा कोई कब्ज़ा कर ले और कभी न वापस करे।''
कथानक से जुड़ पाने का महत्व एक और अनुभव से स्पष्ट हुआ था। एक बार एक प्रशिक्षण सत्र में हमने प्रशिक्षणार्थियों से पूछा कि पर्यावरण आधारित शिक्षण से क्या समझते हैं। एक व्यक्ति ने कहा - उदाहरण के लिए अगर आप एक कहानी सुनाएं कि दो हजार साल पहले एक राजा था, जिसका नाम फलां-फलां था ... उसके दो बेटे थे ... उनमें इस बात पर झगड़ा हुआ कि पिता की मौत के बाद राज्य किस को मिलेगा . उनके बीच युद्ध होता है जिसमें रथों, भालों का इस्तेमाल होता है। तो अब बच्चों ने क्या रथ व भाले देखे हैं? दो हजार साल पहले का समय देखा है? ये बातें तो उनके परिवेश से जुड़ी नहीं हैं। हमने इसी उदाहरण का विश्लेषण किया। सभी से कहा कि ध्यान से हर पंक्ति के भाव को समझें और बताएं कि इसमें से कौन-सा भाव बच्चों के परिवेश में नहीं है?
‘दो हजार साल पहले' यानी कितने समय पहले यह बच्चे कल्पना नहीं कर पाएंगे। यह ठीक बात थी। इसके बाद - राजा, जो एक पिता है, के दो पुत्र हैं ... यह तो परिवेश में मौजूद है ... दो पुत्र पिता की संपत्ति को लेकर स्पर्धा करते हैं ... यह भी परिवेश में मौजूद है। रथ और भाले आज इस्तेमाल नहीं होते - पर बच्चों के सांस्कृतिक परिवेश में ये भी मौजूद हैं - पौराणिक कथाओं में, मन्दिरों में, कैलेंडरों में बने चित्रों में, रामलीला की झांकियों में।... फिर ऐसी एक कहानी पर्यावरण आधारित नहीं है - यह, किस कारण से माना जाता है?
प्रशिक्षणार्थी काफी गहरी सोच में पड़ गए थे। पर्यावरण में क्या नहीं है, इसकी सूची बनाई तो बड़ी चुनिंदा चीजें उसमें आईं .... महाद्वीप, महासागर, पृथ्वी की गतियां, ब्रह्मांड, पृथ्वी कैसे बनी, पहाड़ कैसे बने? पांच हजार साल - दस लाख साल पहले की धारणा ...। इन चुनिंदा चीज़ों पर कैसे व कब बात करनी चाहिए, यह खास शोध व अध्ययन का मसला है।
एक और अनुभव है। एक बार कक्षा तीन के लिए भाषा-पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक तैयार की जा रही थी। उसमें टोलस्टॉय की एक छोटी-सी मार्मिक कहानी का चयन हुआ। कहानी है - गुठली। एक पिता है जो अपने बच्चों के लिए आलू-बुखारे ला कर रखता है और खाने के बाद सब मिल कर खाएंगे यह तय होता है। सबसे छोटा बालक अपना लालच नहीं रोक पाता और चोरी छिपे एक आलू बुखारा खा लेता है। जब सब खाने को बैठते हैं और पिता देखते हैं कि एक फल कम है तो पूछताछ करते हैं। सब मना करते हैं और छोटा बालक भी झूठ बोल देता है कि उसने नहीं खाया। पिता कहते हैं कि उन्हें सिर्फ यह चिन्ता है कि खाने वाले ने गुठली तो नहीं निगल ली - क्योंकि गुठली खाने पर व्यक्ति मर जाता है। छोटा बालक घबरा कर कह उठता है कि उसने गुठली तो खिड़की के बाहर फेंक दी थी। चोरी और झूठ पकड़ा जाता है - सब हंस पड़ते हैं। छोटा बालक झेंप कर रो पड़ता है।
अब बताइए यह कहानी पर्यावरण आधारित है या नहीं? इसके कथानक में कौन-सी बाते हैं जो हम सब के अनुभव लोक में नहीं पाई जाएंगी? शायद सिर्फ एक चीज़ - फल का नाम - आलू-बुखारा। नहीं तो, एक छोटे बच्चे के मन का लालच, चोरी, झूठ, झेप - किसके जीवन का सत्य नहीं है? किताब बनाने के काम में जुटे लोगों के बीच बड़ी घमासान बहस हुई कि क्या आलू-बुखारा शब्द हटाकर चीकू डाल देना चाहिए - ताकि कहानी पूरी तरह पर्यावरण आधारित हो जाए? क्या गारंटी है कि तीसरी कक्षा पढ़ने वाले हर छात्र ने चीकू देखा और खाया होगा? या हर शिक्षक ने ही? अगर ऐसी एक बात भी नहीं आनी चाहिए जो कम से कम शिक्षक ने न देखी हो तो क्या ताजमहल या अमरकंटक पर कभी पाठ नहीं होगा? और अगर ताजमहल पर पाठ हो सकता है तो गुठली कहानी में फल का नाम आलू-बुखारा ही क्यों नहीं रह सकता?
वोई-वोई ...
पर्यावरण अध्ययन को लेकर एक असमंजस का भाव कई लोगों के बीच देखने को मिला। एक स्वैच्छिक संस्था के शिक्षकों की बैठक में भाग लेने का मुझे एक बार मौका मिला था। उन लोगों का प्रयास था कि किसी एक पाठ्यपुस्तक पर निर्भर होकर शिक्षण कार्य नहीं किया जाना चाहिए - संदर्भ पुस्तकालय की पुस्तकों से सामग्री जुटा कर पर्यावरण अध्ययन का काम किया जाना चाहिए। बल्कि सबसे पहले बच्चों से ही जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए।
एक शिक्षक ने एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव सुनाया। वे तीसरी कक्षा पढ़ा रहे थे। उनका कहना था. “थोड़े समय बाद बच्चे पर्यावरण की कक्षा में बोर होने लगते हैं। जब हम उनसे उनके आसपास की बातें पूछते हैं तो वे कहते हैं कि सर यही सब तो पिछले साल भी पूछा था। 'वोई-वोई बातें पूछते हो आप तो। इस कक्षा में कुछ खेल करवाओ न।' तब हम पर्यावरण में उपलब्ध खेल आदि बच्चों को करवाते हैं। इससे पर्यावरण वाली बात भी हो जाती है - और बच्चों में रुचि भी बनी रहती है।''
चर्चा हुई कि बच्चों से ‘वोई-वोई' जानकारी क्यों पूछनी पड़ती है? शिक्षकों ने अपना अनुभव बताया कि मान लो ईधन पर बात कर रहे हैं। तेल है या कोयला है ... इसके बारे में कुछ ज्यादा बात या नई बात करनी हो तो वे बातें बच्चों को तो मालूम नहीं होतीं हैं, हमें भी नहीं मालूम होतीं। सन्दर्भ पुस्तकों से ढूंढ सकते हैं पर अक्सर शिक्षकों की तैयारी नहीं हो पाती। तब बच्चे कहते हैं कि बार बार वही बातें क्यों पूछ रहे हो - हमें खेल ही खिला दो। पर्यावरण अध्ययन में क्या करना चाहिए हमें समझ में नहीं आता।
अलग-अलग आयाम ....
इन सारे अनुभवों से गुजरने के बाद हमारी क्या समझ बन सकती है? पर्यावरण शिक्षा से जुड़े अलग अलग आयाम नज़र आते हैं।
जहां हम अपने समाज को जानने समझने की नई विधियां सीखना चाहते हैं या अपने पर्यावरण के विकास के रास्ते खोजना चाहते हैं वहां स्थानीय जानकारी का इस्तेमाल बहुत प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। पर उतना ही जरूरी और महत्वपूर्ण है समाज के बारे में नए अनुभवों का परिचय प्राप्त करना, इंसानी जिंदगी की विभिन्नताओं का अनुभव लेना - जिसके लिए दूसरे समाज, स्थान या समुदाय की जानकारी अत्यन्त जरूरी हो जाती है।
और जैसा कि हमने पहले कहा है ‘दूसरे' पर्यावरण की जानकारी से जुड़ना, उसे समझना अपने आप में मुश्किल नहीं हो सकता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम वह जानकारी किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या हम लंबी-लंबी सूचियां, पारिभाषिक बातें, अमूर्त शब्दावली, असंबद्ध जानकारी के टुकड़े समेट कर पाठ लिख रहे हैं - या एक सरस कथानक-सा पाठ लिख रहे हैं? सही मानिए - अपने ही गांव मोहल्ले की जानकारी नीरस, अर्थहीन ढंग से लिखी हुई मिले तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह भ्रम हम न पालें कि अपने गांव, अपने जिले, अपने राज्य की बातें पहले बताएं तो सही शैक्षिक सिद्धांत का पालन कर रहे होंगे। लोगों के जीते जागते ठोस अनुभव हों तो हमारे जीवन्त अनुभवों से कैसे नहीं जुड़ेंगे भला?
फिर वो बात अपने मोहल्ले की हो या ध्रुवीय प्रदेश के इग्लू वासियों की।
रश्मि पालीवालः एकलव्य के सामाजिक अध्ययन शिक्षण कार्यक्रम से संबद्ध।


