के. आर. शर्मा


इसी दरम्यान मुझे पता चला कि शहर की एक प्रतिष्ठान कॉलोनी में सरकारी स्कूल था जिसको शिक्षा विभाग को बंद करना पड़ा, “क्योंकि सरकारी स्कूलों में रखा क्या है।”
मन में यह सवाल बरकरार था कि आखिर सरकारी स्कूलों की पढ़ाई के तौर-तरीकों में तो कोई फर्क है नहीं और प्राइवेट स्कूल अंग्रेज़ी का राग अलापाते हैं। खैर सरकारी स्कूलों में देखी-समझी अव्यवस्था के चलते हमने तय किया कि किसी प्राइवेट स्कूल में ही बच्ची को भर्ती कराना उचित होगा और शहर की एक अच्छी समझी जाने वाली स्कूल में हमने अपनी बेटी ‘सोनू’ को भर्ती करा दिया।
घर का नाम सोनू, बाहर कानाम श्रुति। स्कूल में बच्ची के इन्टरव्यू के दौरान एच.एम. (हेडमास्टर) से काफी बतिया रही थी। वो। सोनी का एडमिशन हो गया। नियम कानूनों के बारे में एच.एम. ने हमको बताया। कोई दर्जन भर से ज्य़्ाादा नियम कानूनों को पालन करने के लिए हमसे हामी भरवाई गई।
हम कभी नहीं भूल सकते जब साढ़े तीन साल की नन्हीं-सी जान स्कूल जाने के लिए लातायित थी। हमारे आगे-आगे भागी जा रही थी। उसने अपने बस्ते में कुछेक खिलौने रखे हुए थे। शायद सोचा होगा कि स्कूल में खेलने-कूदने को मिलेगा।
स्कूल पहुंचने पर उसकी टीचर ने हमको किताबों की एक लंबी फेहरिस्त थमा दी। बच्ची को टीचर के सुपुर्द किया। टीचर ने बच्ची का बस्ता देखा, हमको वापस बुलाया और उसके बस्ते के खिलौने हमको यह कहकर दे दिए कि यहां इनकी ज़रूरत नहीं। वह अपने चहेते खिलौनों से जुदा नहीं होना चाहती थी, उसने जिद भी की।
बहरहाल बस्ते में खिलौनों की जगह किताबों ने ले ली।
शाम का समय - सोनू स्कूल से घर लाई जा चुकी है। हालांकि बस्ते में नई-नई किताबें भरी थीं, किंतु उसने शाम को बस्ते की तरफ देखा भी नहीं और अपने खिलौनों में मशगूल हो गई।
दूसरे दिन वह स्कूल जाने के नाम पर सिसकते हुए बोली - मैं स्कूल नहीं जाऊंगी।
“क्यों नहीं जाओगी? उसकी मां ने पूछा।”
“स्कूल तो गंदी है ... नहीं जाऊंगी।”
“टीचर डांटती है।”
“लिखने को कहती है टीचर।”
“वहां खेलने नहीं देते।”
“मेरी दोस्त से बात भी नहीं करने देती। हम सबको मुंह पर ऊंगली रखने को कहती है।”
टुकड़े-टुकड़े में उसने सब कुछ बताया और वह फिर खेलने में व्यस्त हो गई।
सोनू स्कूल न जाने की हर संभव कोशिश करती है। अक्सर वह स्कूल जाने के समय हमारे पड़ोसी के घर चली जाती है। पर उसको स्कूल तो जाना ही है। पर उसको स्कूल तो जाना ही है। ज़बरदस्ती सोनी को स्कूल भेजा जाता है।
कुछ ही दिनों में हमको अहसास हो गया कि स्कूल बच्ची को खुशियां प्रदान नहीं कर पाएगा। हम यह तो समझते हैं कि हर काम में खुशियां नहीं मिलतीं। और बच्चों को कठिन काम भी सौंपने चाहिए, पर उन कामों में चुनौतियां होनी चाहिए। हकीकत यह है कि स्कूल में बच्चों को चुनौतियां नहीं परोसी जाती।
एक दिन मैं सोनू से पूछता हूं, “स्कूल में तुमको क्या अच्छा लगता है?”
वह कहती है, “कुछ भी नही।” “फिर भी, तो अच्छा लगता होगा?”
वह थोड़ा सोचती है, और कहती है, “हां, क्लास के बाहर मैदान में कुत्ते के छोटे-छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं? पर टीचर तो खिड़की में से बाहर देखने भी नहीं देती!”
रोज़ का सिलसिला बन पड़ा था - सोनी का स्कूल जाने के दौरान रूठना, बहाने बनाना! वह दूसरी कक्षा में प्रवेश पा चुकी थी।
एक दिन जो वाकिया हुआ उसने हमारे दिलो-दिमाग को हिलाकर रख दिया। शाम को सोनू स्कूल से घर आती है। उसका खाने का डिब्बा ज्यों-का-त्यों है। पूछने पर बताती है टीचर ने नहीं खाने दिया।
क्यो?, सोनू की मां ने पूछा।
इस क्यों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन हम टीचर से मिले।
पूछने पर टीचर ने कहा, “देखिए जो लिखने को दिया था वह इसने नहीं लिखा। इसलिए इसको खाना नहीं खाने दिया।” (हमने देखा कि कक्षा में 8-10 नन्हें बच्चें बेंच पर खड़े हैं।)
हमने पूछा कि बच्ची ने लिखा नहीं इसलिए उसको दोपहर के खाने से वंचित रखना कहां का तर्कसंगत है? क्या उसको खाना नहीं खाने देने से वह लिखेगी?
टीचर बड़े गुस्से में बोली, देखिए यह सब तो करना पड़ता है और मैंने उसकी पिटाई तो नहीं की है। थोड़ा-सा तो डराना पड़ता है।
दरअसल अच्छे-से-अच्छे समझे जाने वाले स्कूलों में भी छात्रों को किसी-न-किसी प्रकार की सज़ा दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिना सज़ा के बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता? जबकि सच्चाई तो यह है कि स्कूल की पढ़ाने की प्रक्रियाएं सहज और रूचिकर नहीं होती और इस वजह से बच्चे ऊबने लगते हैं, शरारत करने लगते है बच्चों को कक्षा की दीवार पर लगे ब्लैक बोर्ड पर फूल पत्ती का चित्र बनाकर पढ़ाया जाता है। जबकि खिड़की में हाथ डालकर पत्ती तोड़ी जा सकती है।

तीसरी में ही विज्ञान विषय में पेड़ के बारे पढ़ाया जाता है। एक दिन सोनू ने घर आकर बताया कि पापा पौधे के बारे में टीचर में होमवर्क दिया है। होमवर्क कॉपी में चित्र बनाने के पहले मैंने छोटा5सा पौधा उखाड़ा और उसको बताया। अनेक सवाल-जवाब हुए। और फिर उसने कॉपी में उस पौधे का चित्र बनाया। टीचर ने सब कॉपी जांची तो पौधे के चित्र के चित्र को काट दिया। इसलिए क्योंकि किताब में और उसकी कॉपी में बने चित्र में फर्क था। कॉपी में बनाया चित्र था तो पौधे का, पर उसकी पत्तियां लंबी न होते हुए गोलाई लिए हुए थीं। उसने जो देखा था हुबहू बना डाला था इस वजहसे कॉपी में नोट मिला कि फिर से चित्र बनाओं। ऐसे और भी कितने ही मामलों में हमने सोनू को अपने आसपास की चीज़ों को देखने के लिए प्रेरित किया किंतु नतीजे उल्टे ही निकले। जो किताब में लिखा है बस वही सच है - टीचर कहती है।
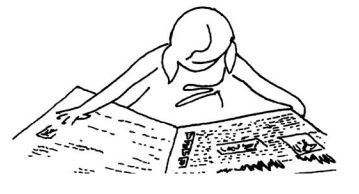
प्राइवेट स्कूलों की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि बच्चे स्कूल के अलावा घर पर भी चैन से नहीं जी सकते। स्कूल से घर आए कि होमवर्क के लिए जोत दिए जाते हैं।
बच्चों को क्या समझ में आया इससे कोई लेना-देना नहीं, होमवर्क पूरा होना चाहिए। और जो पूछा जाए उसका उत्तर दिया जाए - बस। ताकि परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। हमने देखा कि जब सोनू तीसरी कक्षा में थी तब तीन-तीन घंटों तक तो उसको होकवर्क ही करना पड़ता था। यदि होमवर्क नहीं हुआ तो दूसरे दिन डायरी में एक लंबा-सा नोट पालक के लिए भेजा जाता है।
मैं सोचता हूं कि प्राइवेट स्कूल किस मायने में बेहतर होते हैं?क्या यहां के शिक्षकों का शैक्षिक स्तर यहां की शिक्षण पद्धति सरकारी स्कूलों से फर्क होती है! हम पिछले कुछ वर्षो से देख रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं। प्राइवेट स्कूलों में तो अंग्रेज़ी का बोलबाला होता है फिर भी सरकारी स्कूलों की शिक्षकों से शैक्षिक स्तर पर प्राइवेट स्कूल के शिक्षक बेहतर नहीं दिखे। न ही पढ़ाई के तौर तरीकों में बुनियादी फर्क दिखा। बल्कि एक चीज़ ज़रूर दिखी कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बस्ते का बोझा अधिक है। पाठ्य-पुस्तक निग की पुस्तकों के अलावा दिल्ली-कलकत्ते के निजी प्रकाशनों की मंहगी किताबें बस्ते का बोझ बढ़ा देती है।
अच्छे स्कूल समझे जाने वाले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बस्ते भारी भरकम होते हैं, वहां अनुशासन का कहीं ज़्यादा दबदबा होता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं - स्कूल के माहौल को एकदम असहज बनाने की भरपूर कोशिश होती है। शायद बच्चों को चारदीबारी में बंद करके उनको उबाने में स्कूल को आनंद और संतोष मिलता है। बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उनको शारीरिक दंड मिलता है या उनके साथ जो बर्ताव होता है, वह भी अक्सर हिंसात्मक होता है।
सोनू को स्कूल जाते हुए छह साल हो चुके हैं। इस दौरान हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि चाहकर भी घर पर सीखने की प्रक्रियाओं पर ज़ोर नहीं दे पाते हैं। क्योंकि हमें बच्ची को वह सब कुछ प्राथमिकता के आधार पर कराना होता है जो स्कूल चाहता है। स्कूल में प्रतिस्पर्धा का ज़बरदस्त बोलबाला है। पल-पल में प्रतिस्पर्धा है। यहां तक कि बाल सभा जो कि स्कूल का अनौपचारिक कार्यक्रम होना चाहिए, वहां भी हर बच्ची बच्चे को बोलने की छूट नहीं दी जाती और वातावरण इस तरह बनता है कि उनमें ईष्र्या भी भावना पैदा कर दी जाती है कि मैं फलां से बेहतर हूं।
हमने अहसास किया कि सोनी जब अपनी मर्जी से पढ़ने बैठती है या हमसे पढ़ना चाहती है तो उसके जेहन में एक ही बात होती है कि उसने पढ़ाई नहीं की तो कम नंबर आएंगे, वो ‘फेल हो जाएगी’, ‘टीचर जी डांटेंगी’ वगैरह-वगैरह! और इस चक्कर में उसकी जिज्ञासाकों का दमन होता जा रहा है। वह स्कूल में तो सवाल पूछ नहीं सकती पर घर में चाहकर भी नहीं पूछती क्योंकि उसको पढ़ाई जो करनी है।
कुल मिलाकर स्कूल बच्चों में यह भावना पनपाते हैं कि स्कूल में जो कुछ भी वे करते हैं उसका लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक पाने से ज़्यादा कुछ नहीं।

अपने देश में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते। उसका कारण उन बच्चों के परिवार की आर्थिक या पारिवारिक परिस्थितियों का महज प्रतिकूल होना नहीं बल्कि स्कूल का माहौल भी शायद एक कारक है उसमें। बच्चा आखिर स्कूल क्यों जाए?
(के.आर.शर्मा - एकलव्य के होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण, कार्यक्रम से संबद्ध, उज्जैन केंद्र में कार्यरत।) रेखा चित्र: उमेश गौर


