मुकेश मालवीय
चित्रः विप्लव शशि
कुल कक्षाएं पांच--- एक से पांचवीं तक; और शिक्षक एक। ऊपर से सरकारी काम भी करना है। तो कैसे चले शिक्षा की बात। और अगर शिक्षक संवेदनशील हो, जो शिक्षा कैसे दी जानी चाहिए जैसे सवाल पर सोचता हो तो मामला और भी दुविधाजनक। लेकिन कुछ तो तरीके फिर भी खोजे जा सकते हैं।

पिछले लगभग सात वर्षों से मेरी शाला एक शिक्षकीय शाला रही है। कक्षाएं पहली से पांचवीं तक, और बच्चे 100 से 150 के बीच। सारे इतर शैक्षणिक काम करते हुए मैं कुछ वक्त अपनी इन कक्षाओं को समझने और समझाने के लिए भी निकाल सका। इसलिए यह अनुभव एक व्यवस्था की देन है, मेरे शिक्षण की वकालत नहीं।
एक दृश्य
तीन कमरों में पांच कक्षाएं बैठती हैं। शुरू में हर कक्षा की एक अलग पंक्ति होती थी, परन्तु एक कमरे में बैठी दोनों कक्षाओं के बच्चे एक साथ एक ही काम करते थे; जैसे कि दूसरी के बच्चे अगर गिनती लिखते तो पहली के बच्चे भी लिखने लग जाते। चौथी के बच्चे अगर किताब पढ़ते तो तीसरी के बच्चे भी अपनी किताब खोलकर पढ़ते या पढ़ने का अभिनय करते।
खेलते समय ये बच्चे न तो कक्षा का बन्धन स्वीकार करते न उम्र का। धीरे-धीरे यह बात कक्षा में भी दिखने लगी। एक कमरे में बैठी दोनों कक्षाओं के बच्चे आपस में मिलकर बैठने लगे। मैंने न तो उन्हें अलग-अलग पंक्तियों में, कक्षावार बैठने को कहा था और न ही इस तरह मिलजुल कर। कुछ दिनों बाद मैंने एक सत्र में बार-बार इन कक्षाओं का बदलाव किया - कुछ समय पहली और तीसरी के बच्चे एक साथ बैठते तो कुछ समय बाद तीसरी और पांचवीं के बच्चे। यानी एक सत्र में हर कक्षा अन्य सभी कक्षाओं के साथ कुछ समय तक ज़रूर बैठ चुकी होती। 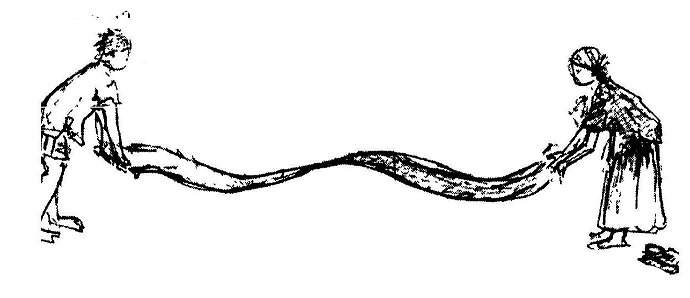 सीखने की प्रेरणा और परस्पर शिक्षण
सीखने की प्रेरणा और परस्पर शिक्षण
इन वर्षों में मैंने अनुभव किया कि बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं वह स्वयं उनकी कुछ जानने और करने की इच्छा के कारण है; और इस इच्छा को प्रेरित करते हैं वे बच्चे जो कुछ अधिक सीखे हुए हैं। कक्षा चौथी के बच्चे को किताब पढ़ते देख कक्षा दो के बच्चे का किताब पढ़ने का अभिनय उसे उतना ही आनन्द देता है, जितना किताब पढ़ने वाले को। अगर इस तरह की प्रेरणा न हो तो मुझे लगता है कि पढ़ना सीखना या कुछ भी सीखना-सिखाना मुश्किल है। इस प्रेरणा और इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए सीखने का एक माहौल एवं परिस्थिति उपलब्ध कराने का एक प्रयास मैंने भी किया।
 नियंत्रण में ढील
नियंत्रण में ढील
शासन एवं शिक्षकीय नियंत्रण को बहुत कम करनाः बच्चों की स्वतंत्रता मेरी पहली मजबूरी थी - एक साथ इतने बच्चों पर नियंत्रण रखने के साथ उन सरकारी कामों को करना संभव नहीं था जो मुझसे अपेक्षित थे। पर यह भी आवश्यक था कि इस स्वतंत्रता से अराजकता पैदा न हो। कुछ समय के अनुभवों के बाद यह लगा कि बच्चों के काम और जिम्मेदारी पहले से तय होनी चाहिए। अब मैं हर दिन बच्चों से क्या करवाना है यह तय करता। लेकिन उस काम के सही क्रियान्वयन के लिए मेरी उप स्थिति जरूरी बन जाती। इसी दौरान छोटे-छोटे समूहों में काम (गतिविधियां) करवाना बड़े बच्चों से मॉनिटरिंग करवाना आदि कई विकल्प उभरे परन्तु बच्चों की मुझ पर निर्भरता कम नहीं हुई। बच्चों की शिक्षक के प्रति निर्भरता को कम करने के बारे में मुझे फिर से सोचना पड़ा।
मुझे लगा कि बच्चों को क्या सीखना चाहिए यह काम मेरे द्वारा तय हो रहे थे तो स्वाभाविक है कि इसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर थी कि वे सही सीखें। यह सही सिखाने की समझ के कारण मेरी क्रियाशीलता कक्षा में ज़्यादा थी। मैंने इस जिम्मेदारी को विस्थापित करने का सोचा। सीखने के लिए बच्चों को ही ज़िम्मेदारी सौंप रहा था तो ज़ाहिर है कि मेरे अधिकार भी बच्चों को दिए जाने चाहिए थे।
सबसे पहले मैनें बच्चों को शाला संचालन का अधिकार दिया। शाला की सफाई, प्रार्थना, बैठने की व्यवस्था, छुट्टी एवं घंटी बच्चों की सामूहिक भागीदारी से सम्पन्न होती। ऐसा पहले भी होता था पर अब फर्क यह था कि जवाबदेही बच्चों की थी।
इसके साथ ही बच्चों के आपसी विवाद हल करने के लिए भी कक्षा जिम्मेदार थी। इसके लिए मुझ तक आने की आवश्यकता नहीं थी। हां, शुरुआत में कुछ दिन मैंने बच्चों के साथ मिलकर ऐसे मामले निपटाए थे, जिसमें गलती किसकी है यह ढूंढना, और फिर सामूहिक राय से सजा तय करना शामिल था।
मध्यान्ह भोजन को बनावाने की जिम्मेदारी, उसके लिए तेल गुड़ लाने, दलिया पिसवाने एवं हिसाब रखने की जिम्मेदारी भी बच्चों पर थी। हां, पर अधिकारियों को दिखाने के लिए मुझे अलग से हिसाब रखना पड़ता।
इसी दौरान शाला में परस्पर शिक्षण का एक माहौल बना। मैंने यह प्रयास किया कि अधिक जानने वाले बच्चे अन्य बच्चों को सिखाने और समझाने के लिए जिम्मेदार हों। जैसे कि पढ़ना जानने वाले हर बच्चे के साथ ऐसे दो-दो बच्चों का बंटवारा किया गया जो पढ़ना नहीं जानते थे। ये बच्चे उन्हें नकल लिखकर लाने को कहते उंगली रखकर पढ़ाते, शुद्ध-लेख लिखवाते, और मुझसे शिकायत भी करते अगर बच्चे काम करके नहीं लाते। इसी तरह जोड़ना सिखाने वाले, घटाना सिखाने वाले बच्चों के समूह बनाए गए। कक्षा के हर बच्चे को जोड़ना या घटाना सिखाने की जिम्मेदारी इन टीमों को दी गई। साथ ही टीम एवं उनके दायित्व बदलते रहने की प्रक्रिया भी चलती रहती।
स्कूल में बहुत सारी शैक्षणिक सहायक सामग्री बच्चों के बीच उपलब्ध थी। जैसे पुस्तकालय की किताबें, संख्या कार्ड, शब्द कार्ड, चित्र कार्ड, शैक्षणिक चार्ट, हेन्डलेन्स, दर्पण आदि। इनके उपयोग एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी भी बच्चों को दी गई।
यहां मैं यह दावा नहीं करता कि इस सब से सीखना-सिखाना बड़ी तेजी से हुआ, परन्तु परस्पर सहयोग एवं शिक्षण की संस्कृति शाला में ज़रूर पनपी। यह मेरे लिए काफी उत्साहजनक एवं सर्वथा नवीन थी।  शिक्षक-सा कोई स्रोत
शिक्षक-सा कोई स्रोत
कुछ समय बाद मुझे अनुभव हुआ कि बच्चों के पास जितना और जो कुछ है वह तो आपस में बंट रहा है, कुछ थोड़ा इधर-उधर से भी शाला में आ रहा था। उन्हें थोड़ी बहुत मेरी मदद भी मिल रही थी। परन्तु इसके अलावा शिक्षण हासिल करने का कोई और स्रोत भी होना चहिए, जो हर बच्चे के पास एक शिक्षक की तरह उपलब्ध हो।
हर बच्चे के पास एक शिक्षक का होना एक अन्य मायने में जरूरी है। मुझे यह विकल्प पाठ्यपुस्तकों में नज़र आता है। मगर एक तो जिस प्रचलित तरीकों से बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता रहा है उसमें ये पुस्तकें मददगार ( शिक्षक ) नहीं बन पाई दूसरा पाठ्यपुस्तकों को शिक्षक के विकल्प के रूप में बनाया ही नहीं गया।
मैं जिस शाला में पढ़ा रहा हूं वहां ‘एकलव्य' संस्था की ‘खुशी-खुशी' किताबें चलती हैं। ये किताबें अन्य प्रचलित पाठ्यपुस्तकों से भिन्न हैं (मेरी यह समझे इन्हीं किताबों से बनी।)
बच्चों द्वारा इन किताबों को पढ़ने और समझने के लिए शिक्षक की जरूरत को कम से कम किया जा सकता है - अगर पढ़ना सिखाने की कुछ बुनियादी प्रक्रियाओं को बदला जाए तो।
पहला तो यह कि जिस वर्णमाला पद्धति से बच्चे पढ़ना सीखते हैं उससे काफी लम्बे समय तक (करीब पांचवीं तक ) लिखी हुई बात को अर्थों के साथ नहीं पढ़ पाते। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि लिखा हुआ वे जो पढ़ रहे हैं वह उनसे या उनके लिए ही कहा जा रहा है। चलिए इस पहलू को और थोड़ा समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। मैंने तीसरी के उन बच्चों से कुछ सवाल जवाब किए जो पढ़ना जानते थे।
1. मैंने मौखिक रूप से बच्चों को बताया - ‘मोहन को बाज़ार में एक पेन मिला।'
फिर उनसे प्रश्न किया, ‘मोहन को पेन कहां मिला?'
बच्चों का मौखिक उत्तर: ‘बाज़ार में।'
2. मैंने बोर्ड पर लिखा : ‘आशा और बीजू बाज़ार गए थे।'
प्रश्नः ‘आशा और बीजू कहां गए थे?'
फिर बच्चों से कहा कि बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़ो और प्रश्न का उत्तर दो।
बच्चों ने (ज्यादातर ने ) दोनों लाइनें वैसी ही उतार दी।
मैंने पहली लाईन को जोर से पढ़ा और मिटा दिया और फिर कहा दूसरी लाइन पढ़ो और जवाब लिखो।
कुछ बच्चों ने लिखाः ‘आशा और बीजू कहां गए थे।'
कुछ ने लिखाः ‘आशा और बीजू कहां गए थे। बाज़ार गए थे।'
कुछ ने लिखाः ‘बाजार गए थे।
दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मेरी समझ में आई कि बच्चे काफी लम्बे समय तक लिखी हुई भाषा को अलग और बोलने वाली भाषा को अलग मानते हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि जो बोला जाता है वही लिखा भी जाता है और इस अविश्वास को बनाने का काम भी पाठ्यपुस्तकें ही करती हैं। क्योंकि पढ़ना सीखते समय जिस लिखित भाषा से उसको सामना होता है, उसमें उसकी बोलचाल की भाषा के अंश काफी कम होते हैं।
 पाठ्यपुस्तकों को बच्चों के समझने की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए जरूरी था कि बच्चे सार्थक सन्दर्भों से पढ़ना सीखें। दूसरा अपनी बात लिखकर अभिव्यक्त कर सकें और लिखी हुई बात को अपनी बात समझा सकें।
पाठ्यपुस्तकों को बच्चों के समझने की दृष्टि से उपयोगी बनाने के लिए जरूरी था कि बच्चे सार्थक सन्दर्भों से पढ़ना सीखें। दूसरा अपनी बात लिखकर अभिव्यक्त कर सकें और लिखी हुई बात को अपनी बात समझा सकें।
इसके लिए मेरा पहला प्रयास तो यह था कि वर्णमाला रटने को बढ़ावा नहीं दिया गया। इसकी जगह छोटी कविताओं को कार्डशीट पर लिखकर कक्षा में टांगा गया। इन कविताओं को बच्चों ने जल्दी ही याद कर लिया। इन कविताओं में लाइनों को पहचानना, शब्दों को पहचानना जैसी गतिविधियां हुई। किसी शब्द की पहचान होने के बाद उसके पहले या बाद में कौन-सा शब्द आया है इसे पहचानना। जैसे अगर बोर्ड पर लिखा हो
"चुपके-चुपके आती नींद"
इसे एक-दो बार मैंने पढ़ के बता दिया। इसमें नींद चूंकि अतिंम शब्द है। इसलिए इसे पहचानना मुश्किल नहीं होता। अब अगर पूछा जाए कि नींद के पहले कौन-सा शब्द लिखा है - इसके लिए पहले तो बच्चा उस शब्द पर उंगली रखे जो नींद के पहले लिखा है; और फिर सोच कर बताए कि यह कौन-सा शब्द है - बच्चे मन में यह लाईन दुहराते और इस शब्द की पहचान करते।
इसी तरह कई अन्य लिखित संदर्भ लेकर, शब्द कार्डों की मदद से, शब्दों की तुकबन्दी करके, किसी अक्षर विशेष से प्रारम्भ होने वाले शब्दों को इकट्ठा करके, शब्दों को ध्वनियों में तोड़कर पढ़ना सीखने-सिखाने की शुरुआत हुई।
इस पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण यह था कि बच्चों की अपनी समझ की इस तरह पढ़ने में पूरा इस्तेमाल हो रहा था। सोचना, तय करना, किसी नतीजे पर पहुंचना आदि - उस समय बच्चों का उत्साह देखते ही बनता।
मेरा दूसरा प्रयास उन बच्चों के साथ था जो पढ़ने की कोशिश कर रहे थे या पढ़ तो लेते थे, पर पढ़ी हुई सामग्री से अर्थ नहीं निकाल पाते थे। मुझे लगा कि ऐसे बच्चे अगर उन बातों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करें जो वह दोस्तों से या माता पिता से करते हैं, तो उनका लिखने और बोलने की भाषा से संबंध बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने कुछ इस तरह के कदम उठाएः
1. डेली डायरी: कक्षा तीसरी से पांचवीं तक के हर बच्चे को अपने दैनिक क्रियाकलाप की एक डायरी लिखना होती। स्कूल में उन्होंने क्या-क्या किया; स्कूल से घर जाने के बाद और फिर स्कूल आने के बीच उन्होंने जो कुछ भी किया, वे डायरी में लिखकर लाते। कुछ दिनों बाद इस डायरी में काम के अलावा आस-पास की खबरों को भी शामिल किया गया - जैसे कि उस दिन मोहल्ले में क्या हुआ, किसके यहां मेहमान आए, किसका झगड़ा हुआ आदि, आदि।
शुरू की डायरियां देखें तो वो अधूरे वाक्यों, मात्राओं की गलती एवं एक जैसे वाक्य में लिखी गई थीं। जैसे कि मैं खेत गया, मैं नदी गया, मैं रोटी खाया, आदि। कुछ डायरियों में जो लिखा था उसे पढ़ना मुश्किल था, परन्तु पेज भरा हुआ था। कुछ डायरियों में कुछ शब्द पढ़ने में आते थे, तो एक अनुमान लगाया जा सकता था कि क्या कहने की कोशिश की गई है।
कुछ दिनों तक इन डायरियों को देखने के बाद मैंने बच्चों से कहा कि अब अपनी-अपनी डायरियों को पढ़के भी सुनाना होगा। डायरी पढ़वाने से मुझे दो-तीन बातें समझ में आईं। एक तो जिनकी डायरी पढ़ने में नहीं आ रही थी, वे बच्चे उसे खुद अन्य पढ़ने वाले बच्चों की तरह ही पढ़ रहे थे।
दूसरा, मात्राओं की गलती वाले शब्द कुछ बच्चे तो सही पढ़ते, कुछ उस गलती को पढ़ते, सुधारते और फिर पढ़ते - जैसे कि 'मैंने अगार सिलगाया' को पहले ऐसे ही पढ़ा फिर तुरन्त बाद मैंने अंगार सिलगाया'पढ़ा।
तीसरी बात जो मैंने महसूस की कि बच्चे अपने लिखे हुए को पढ़ते समय अटपटापन महसूस करते थे। उन्हें यह अहसास था कि जैसा वो बोलते हैं लिखा हुआ वैसा नहीं है बल्कि काफी रूखा-सूखा है। इस लेखन में शब्द तो वही थे जो बच्चे बोलते हैं। परन्तु उनका लहज़ा, बोलचाल का तरीका आदि कैसे लिखा जाता?
2 स्वतंत्र लेखनः किसी भी ऐसे विषय पर बच्चों को एक पेज लिखने को कहा जाता जिससे वो परिचित हो - जैसे त्योहार, बाजार, मध्यान्ह भोजन, चुनाव, सरपंच, पल्सपोलियो, गर्मी की छुट्टी आदि। इन विषयों पर बच्चे जो भी लिखते उसे पढ़ा जाता। फिर यह चर्चा होती कि इस विषय पर और क्या क्या लिखा जा सकता था। यह चर्चा आगे के विषयों के लेखन के लिए महत्वपूर्ण होती। फिर बच्चे उस विषय पर सारी संभावनाओं पर सोच कर लिखते।
3 चित्रों पर लेखन: बच्चों को अखबार में छपे या पुस्तकालय की किताबों के चित्र दिए जाते। पहले इन चित्रों पर बातचीत होती। चित्रों पर बातचीत में कल्पनाओं की असीम उड़ान उड़ी जा सकती है। कल्पनाओं को लेखन में उतारने के लिए चित्र उपयोगी माध्यम बन सके।
 4. अखबार कालः चूंकि बच्चों की डायरियों में मोहल्ले की खबरें बहुत आने लगी थीं। तो शाला का अखबार निकालने का विचार आया। इन सारी खबरों को अलग-अलग पेज पर लिखा जाता। इसे एक बड़ी कार्ड शीट पर चिपका कर स्कूल में लगा दिया जाता। ये खबरें पढ़ना सीखने में सहायक बन रही थीं।
4. अखबार कालः चूंकि बच्चों की डायरियों में मोहल्ले की खबरें बहुत आने लगी थीं। तो शाला का अखबार निकालने का विचार आया। इन सारी खबरों को अलग-अलग पेज पर लिखा जाता। इसे एक बड़ी कार्ड शीट पर चिपका कर स्कूल में लगा दिया जाता। ये खबरें पढ़ना सीखने में सहायक बन रही थीं।
कविताओं के लिए चित्र बनानाः मैंने बाल पुस्तकालय की कविताओं की किताबों से कुछ कविताओं को पर उतारा। इन कविताओं को बच्चों को पढ़कर सुनाया। जो बच्चे पढ़ सकते थे उन्होंने भी इन कविताओं को पढ़ा। इसके बाद बच्चों को टोलियों में बांट दिया। हर टोली को कविता की एक कार्डशीट दे दी। बच्चों को इस कविता के आधार पर चित्र बनाने थे। शुरूआत में बच्चों से बातचीत हुई कि कविता में जो कुछ कहा गया है उसको ही चित्र में बनाया जा सकता है। छोटी कक्षाओं के बच्चों ने भी इस गतिविधि में भाग लिया।
लिखित निर्देश देना  यह गतिविधि मौखिक निर्देश से प्रारम्भ हुई। कोई एक विद्यार्थी किसी छात्र विशेष के लिए या सभी के लिए निर्देश देता। निर्देश कुछ ऐसे होते कि जोर-जोर से हंसो या बाहर से नीम की पत्ती लाओ। इसी तरह हर छात्र को कोई न कोई निर्देश देना पड़ता। बाकी उसका पालन करते। इसी प्रक्रिया को बाद में ‘लिखित निर्देश देने में बदल दिया गया। निर्देश को श्यामपट पर या पर्ची पर लिखा जाता।और इस निर्देश का पालन मौखिक या लिखित रूप से करना पड़ता। इन निर्देशों की भाषा धीरे-धीरे बदलती गई। ‘अपना नाम लिखकर बताओ' जैसे निर्देशों से लेकर ‘अपनी किताब का सुखनराम की मौसी वाला पाठ कौन-से पेज पर है। इस तरह के निर्देशों को समझने और उनके अनुसार काम करने से यह विश्वास बनाने में मदद मिली कि जो लिखा हुआ है वह हमसे कुछ कहता है।
यह गतिविधि मौखिक निर्देश से प्रारम्भ हुई। कोई एक विद्यार्थी किसी छात्र विशेष के लिए या सभी के लिए निर्देश देता। निर्देश कुछ ऐसे होते कि जोर-जोर से हंसो या बाहर से नीम की पत्ती लाओ। इसी तरह हर छात्र को कोई न कोई निर्देश देना पड़ता। बाकी उसका पालन करते। इसी प्रक्रिया को बाद में ‘लिखित निर्देश देने में बदल दिया गया। निर्देश को श्यामपट पर या पर्ची पर लिखा जाता।और इस निर्देश का पालन मौखिक या लिखित रूप से करना पड़ता। इन निर्देशों की भाषा धीरे-धीरे बदलती गई। ‘अपना नाम लिखकर बताओ' जैसे निर्देशों से लेकर ‘अपनी किताब का सुखनराम की मौसी वाला पाठ कौन-से पेज पर है। इस तरह के निर्देशों को समझने और उनके अनुसार काम करने से यह विश्वास बनाने में मदद मिली कि जो लिखा हुआ है वह हमसे कुछ कहता है।
पैराग्राफ पर सवाल जवाब: बच्चों को कुछ लिखित पैराग्राफ दिए जाते। साथ में कुछ प्रश्न होते जिनका जवाब उस लिखित अंश में होता। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना - अर्थ के साथ - ज़रूरी होता। इस गतिविधि की मदद से दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बच्चों की समझ बनाने का प्रयास हुआ। पहला तो यह कि जो प्रश्न पूछा गया उसका क्या मतलब है। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसका जवाब क्या होगा। इसके लिए पहले बोल-बोलकर पैराग्राफ पढ़ना, प्रश्न मौखिक पूछना, उत्तर मौखिक देना जैसी गतिविधियां हुईं। फिर लिखित जवाब देने पर जोर दिया गया। इन लिखित उत्तरों पर भी चर्चा होती थी कि जो जवाब लिखे गए क्या वही सही जवाब हैं। या उनके अलावा और कुछ भी लिखा जा सकता था। मुझे लगता है किसी भी बात पर समझ बनाने के लिए उस पर सही चर्चा करना बहुत उपयोगी होता है।
 बालपुस्तकालय की किताबें: गांव में जिस तरह आज भी आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उसी तरह आधुनिक शब्दावली का भी वहां काफी अभाव होता है। एक सीमित शब्दभण्डारे के साथ काम करते हुए लगा कि इस शब्द-भण्डार में वृद्धि के विकल्प कहीं न कहीं ढूढने होंगे। टी. वी., रेडियो, समाचार पत्र, आदि गांव में बहुत कम हैं। गांव की मुख्य भाषा गोंडी होने की वजह से हिन्दी का प्रयोग भी बहुत कम है। जब लोग शहरी बच्चों से इन बच्चों की तुलना करते हैं तब क्या वे भाषा के इस परिवेश पर सोचते हैं। शायद नहीं?
बालपुस्तकालय की किताबें: गांव में जिस तरह आज भी आधुनिक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, उसी तरह आधुनिक शब्दावली का भी वहां काफी अभाव होता है। एक सीमित शब्दभण्डारे के साथ काम करते हुए लगा कि इस शब्द-भण्डार में वृद्धि के विकल्प कहीं न कहीं ढूढने होंगे। टी. वी., रेडियो, समाचार पत्र, आदि गांव में बहुत कम हैं। गांव की मुख्य भाषा गोंडी होने की वजह से हिन्दी का प्रयोग भी बहुत कम है। जब लोग शहरी बच्चों से इन बच्चों की तुलना करते हैं तब क्या वे भाषा के इस परिवेश पर सोचते हैं। शायद नहीं?
मैंने बाल-पुस्तकालय के सही क्रियान्वयन पर ध्यान दिया। हर बच्चे को स्कूल में, घर में ये किताबें ले जाने दी जाती। इन्हें पढ़कर, किताब पर एक पेज लिखकर लाना होता कि किताब कैसी लगी? किताब में किसके बारे में बात की गई है? किताब के चित्र कैसे हैं? किताब की किस बात पर मज़ा आया? इस तरह की एक रिपोर्ट उस किताब पर लिखी जाती। साथ-साथ मैं पाठ्यपुस्तकों के प्रति भी बच्चों का लगाव बढ़ाने में कुछ-कुछ सफल हुआ। पाठ्यपुस्तकों का काफी हिस्सा बच्चे स्वयं एवं आपसी चर्चा से निपटाते। किताब की हर लाईन समझने के लिए शिक्षक की जरूरत कम हुई। शायद शुरू में मैं इसी उद्देश्य को लेकर चला था।
यहां मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि आप यह न माने कि मैं बहुत सफल हूं। ऐसा कहा जाता है कि सफलता के लिए चाहिए एक अलग तरह के बच्चे जैसे हमने अभी तक देखे न हो। पर ये बच्चे अन्य बच्चों की तरह ही हैं। हर बच्चे में विविधता है। और दावे से मैं इनके बारे में एक लाईन भी नहीं कह सकता।
मुकेश मालवीयः बैतूल ज़िले की शाहपुर तहसील के एक गांव पावरझंडा की प्राथमिक शाला में शिक्षक हैं।



